ज्योतिष के विषय में विस्तृत जानकारी
ज्योतिष की परिभाषा एवं ज्योतिष के अंगों के बारे में विस्तृत जानकारी
ज्योतिष विषय वेदों जितना ही प्राचीन है। ग्रह, नक्षत्र और अन्य खगोलीय पिण्डों का अध्ययन करने के विषय को ही ज्योतिष कहा जाता है । इसके गणित भाग के बारे में तो बहुत स्पष्टता से कहा जा सकता है कि इसके बारे में वेदों में स्पष्ट गणनाएं दी हुई हैं। फलित भाग के बारे में बहुत बाद में जानकारी मिलती है।
- १ – वेदाङ्ग ज्योतिष
- २ – सिद्धान्त ज्योतिष या ‘गणित ज्योतिष’
- ३ – फलित ज्योतिष
- ४ – अंक ज्योतिष
- ५ – खगोल शास्त्र
(१) – वेदाङ्ग ज्योतिष
वेदाङ्ग ज्योतिष कालविज्ञापक शास्त्र है।
वेदा हि यज्ञार्थमभिप्रवृत्ताः कालानुपूर्वा विहिताश्च यज्ञाः।
तस्मादिदं कालविधानशास्त्रं यो ज्योतिषं वेद स वेद यज्ञान् ॥
(आर्चज्यौतिषम् ३६, याजुषज्याेतिषम् ३)
चारो वेदों के पृथक् पृथक् ज्योतिषशास्त्र थे। उनमें से सामवेद का ज्योतिषशास्त्र अप्राप्य है, शेष तीन वेदों के ज्योतिष शास्त्र प्राप्त होते हैं।
- (१) ऋग्वेद का ज्योतिष शास्त्र – आर्चज्याेतिषम् (इसमें ३६ पद्य हैं।)
- (२) यजुर्वेद का ज्योतिष शास्त्र – याजुषज्याेतिषम् (इसमें ४४ पद्य हैं।)
- (३) सामवेद का ज्योतिष शास्त्र – अप्राप्य है।
- (४) अथर्ववेद ज्योतिष शास्त्र – आथर्वणज्याेतिषम् (इसमें १६२ पद्य हैं।)
इनमें ऋक् और यजुः ज्याेतिषाें के प्रणेता लगध नामक आचार्य हैं। अथर्व ज्याेतिष के प्रणेता का पता नहीं है।
पीछे सिद्धान्त ज्याेतिष काल मेें ज्याेतिषशास्त्र के तीन स्कन्ध माने गए- सिद्धान्त, संहिता और होरा। इसीलिये इसे ज्योतिषशास्त्र को ‘त्रिस्कन्ध’ कहा जाता है। कहा गया है –
सिद्धान्तसंहिताहोरारुपं स्कन्धत्रयात्मकम्।
वेदस्य निर्मलं चक्षुर्ज्योतिश्शास्त्रमनुत्तमम् ॥
वेदाङ्ग ज्याेतिष सिद्धान्त ज्याेतिष है, जिसमें सूर्य तथा चन्द्र की गति का गणित है। वेदांङ्ग ज्योतिष में गणित के महत्त्व का प्रतिपादन इन शब्दों में किया गया है –
यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा।
तद्वद् वेदांगशास्त्राणां गणितं मूर्धनि स्थितम्॥ (याजुषज्याेतिषम् ४)
अर्थात् जिस प्रकार मोरों में शिखा और नागों में मणि का स्थान सबसे उपर है, उसी प्रकार सभी वेदांगशास्त्रों मे गणित का स्थान सबसे उपर है।
इससे यह भी प्रकट होता है कि उस समय ‘गणित’ और ‘ज्योतिष’ समानार्थी शब्द थे।
वेदांङ्ग ज्याेतिष में वेदाें जैसा (शुक्लयजुर्वेद २७।४५, ३०।१५) ही पाँच वर्षाें का एक युग माना गया है। (याजुष वेदाङ्गज्याेयोतिष ५)
वर्षारम्भ उत्तरायण, शिशिर ऋतु और माघ अथवा तपस् महीने से माना गया है। (याजुष वे. ज्याे. ६)
युग के पाँच वर्षाें के नाम- संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, इद्वत्सर और वत्सर हैं।
अयन दाे हैं- उदगयन (उत्तरायण) और दक्षिणायन।
ऋतु छः हैं- शिशिर, वषन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद् और हेमन्त।
महीने बारह माने गए हैं – तपः (माघ), तपस्य (फाल्गुन), मधु (चैत्र), माधव (वैशाख), शुक्र (ज्येष्ठ), शुचि (आषाढ), नभः (श्रावण), नभस्य (भाद्र), इष (आश्विन), उर्ज (कार्तिक), सहः (मार्गशीर्ष) और सहस्य (पाैष)। महीने शुक्लादि कृष्णान्त हैं। अधिकमास शुचिमास अर्थात् आषाढमास में तथा सहस्यमास अर्थात् पाैष में ही पड़ता है, अन्य मासाें में नहीं।
पक्ष दाे हैं- शुक्ल और कृष्ण। तिथि शुक्लपक्ष में १५ और कृष्णपक्ष में १५ माने गए हैं। तिथिक्षय केवल चतुर्दशी में माना गया है। तिथिवृद्धि नहीं मानी गई है। १५ मुहूर्ताें का दिन और १५ मुहूर्ताें का रात्रि माने गए हैं
वेदाङ्ग ज्योतिष त्रैराशिक नियम
इत्य् उपायसमुद्देशो भूयोऽप्य् अह्नः प्रकल्पयेत्।
ज्ञेयराशिगताभ्यस्तं विभजेत् ज्ञानराशिना ॥
ज्ञानराशि (या, ज्ञातराशि) = वह राशि जो ज्ञात है
ज्ञेयराशि = वह राशि जिसका मान ज्ञात करना है
(२) – सिद्धान्त ज्योतिष
सिद्धांत की दृष्टि से हम ज्योतिष को तीन भागों में बाँट सकते हैं :
(क) स्थितिद्योतक ज्योतिष
(ख) गतिशास्त्रीय ज्योतिष
(ग) भौतिक ज्योतिष
सिद्धान्त ज्योतिष – (क) स्थितिद्योतक ज्योतिष
इसके द्वारा किसी भी खगोलीय पिंड की भूमिस्थित द्रष्टा के सापेक्ष स्थिति को ज्ञात किया जाता है। इसके लिये हम एक भूकेंद्रिक स्थिर खगोल की कल्पना करते हैं। पृथ्वी के अक्ष को यदि अपनी दिशा में बढ़ा दिया जाय तो वह जहाँ पर खगोल में लगेगा उसे खगोलीय ध्रुव कहेंगे। खगोल के उस वृत्त को, जो खगोलीय ध्रुव तथा शिरोबिंदु से होकर जायगा, याम्योत्तर वृत्त कहेंगे। यदि शिरोबिंदु से याम्योत्तर वृत्त के ९०° के चाप दोनों ओर काट लें तो उन बिंदुओं से जानेवाले खगोल के वृत्त को खगोलीय क्षितिजवृत्त तथा याम्योत्तर वृत्त के उस संपात बिंदु को, जो खगोलीय ध्रुव की ओर है, उत्तरबिंदु तथा दूसरी ओर के संपातबिंदु को दक्षिणबिंदु कहेंगे। यदि खगोलीय ध्रुव से याम्योत्तर के दोनों ओर ९०° को चाप काटकर उनसे किसी खगोलीय वृत्त को खींचें, तो उसे खगोलीय विषुवद्वृत्त कहते हैं। सूर्य की दृश्य कक्षा अथवा पृथ्वी की वास्तविक कक्षा को क्रांतिवृत्त कहते हैं। क्रांतिवृत्त तथा खगोलीय विषुवद् वृत्त से २३° २८ का कोण बनाता है। क्रांतिवृत्त तथा खगोलीय विषुवद्वृत्त के संपात को विषुवबिंदु कहते हैं। जिस विषुवबिंदु पर सूर्य लगभग २१ मार्च को दिखाई पड़ता है। उसे वसंतविषुव कहते हैं। किसी भी खगोलीय पिंड की स्थिति उसके निर्देशांकों से ज्ञात हेती है। निर्देशांकों के लिये एक मूल बिंदु, खगोल का वह बृहदवृत्त जिसपर वह बिंदु है, बृहद्वृत्त का ध्रुव, तथा निर्देशांक की धन, ऋण दिशाओं का ज्ञान आवश्यक है। मान लें, हमें किसी तारे के नियामक ज्ञात करने हैं। यदि याम्योत्तरवृत्त तथा खगोलीय विषुवद्वृत्त के ऊपर अभीष्ट तारागामी एक समकोणवृत्त (ध्रुवप्रोत वृत्त) खींचे, तो इस वृत्त पर याम्योत्तर तथा विषुवद्वृत्त के सपात से पश्चिम की ओर धन दिशा मानने पर जितना चाप का अंश होगा वह उसका होरा कोण तथा समकोण वृत्त के मूल से अभीष्ट तारा तक समकोणीय वृत्त (ध्रुवप्रोत वृत्त) के चाप को क्रांति कहेंगे। क्रांति यदि खगोलीय ध्रुव की ओर है तो, धन अन्यथा ऋण, होगी। यदि बसंतविषुव को मूलबिंदु मानें और खगोलीय ध्रुव से विषुवद्वृत्त पर समकोण वृत्त खींचें तो विषुवबिंदु से समकोणवृत्त के मूल तक, घड़ी की सूई की उल्टी दिशा में, जितने चाप के अंश होंगे उन्हें विषुवांश कहेंगे। विषुवांश तथा क्रांति के द्वारा भी खगोलीय पिंड की स्थिति का ज्ञान होता है। यह निर्देशांक पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। यदि शिरोबिंदु से इष्ट खगोलीय पिंड पर समकोण वृत्त खींचे तो उत्तरबिंदु से घड़ी की सूई की दिशा में खगोलीय क्षितिज वृत्त तथा समकोणवृत्त के संपात की दूरी (चापीय अंशों में) दिगंश तथा समकोण वृत्त के चाप की क्षितिजवृत्त से खगोलीय पिंड तक दूरी उन्नतांश होगी। यदि तारा के ऊपर क्रांतिवृत्त के ध्रुव (कदम्ब बिंदु) से एक समकोणवृत्त खींचे तो वह जहाँ क्रांतिवृत से लगेगा यहाँ तक वसंतसंपात से लेकर घड़ी की सूई की विरुद्ध दिशा में क्रांतिवृत्त के चाप के अंशों का भोगांश तथा कटानबिंदु से तारा तक समकोणवृत्त के चाप के अंशों को विक्षेप कहेंगे। इसी धन दिशा क्रांति की तरह होगी। यदि विषुवसंपात के स्थान पर आकाशगंगा के विषुवद् तथा खगोलीय विषुवद का संपातबिंदु लें तथा क्रांतिवृत्त के ध्रुव के स्थान पर आकाशगंगा के विषुवद्वृत्त का ध्रुव लें तो हमें आकाशगंगीय भोगांश तथा विक्षेप प्राप्त होंगे। यदि वसंतविषुव को स्थिर मान लें, तो सूर्य के वसंतबिंदु से चलकर पुन: वहाँ पहुँचने के समय को नाक्षत्र वर्ष कहते हैं। यह ३६५.२५६३६ दिन का होता है। पृथ्वी का अक्ष चल होने के कारण विषुवसंपात प्रति वर्ष ५०.२ के लगभग पीछे हट जाता है। सूर्य के चल विषुवसंपात की एक परिक्रमा के समय को सायन वर्ष कहते हैं। यह ३६५.२४२२ दिन का होता है। वास्तविक सूर्य की गति एक सी नहीं दिखलाई देती। अतः कालगणना के लिये विषुवद्वृत्त में एक गति से चलने वाले ज्योतिष-माध्य-सूर्य की कल्पना की जाती है। उसके एक याम्योत्तर गमन से दूसरे याम्योत्तर गमन को माध्य-सूर्य-दिन कहते हैं। हमारी घड़ियाँ यही समय देती हैं। वास्तवसूर्य तथा ज्योतिष-माध्य-सूर्य के होराकोण के अंतर को कालसमीकार कहते हैं। वायुमंडलीय वर्तन, अपेरण, भूकेंद्रिक लंबन और अयन तथा विदोलन गति के कारण हमें गणित द्वारा उपलब्ध स्थान से आकाशपिंड कुछ हटे से दिखलाई देते हैं। अतः वास्तविक स्थिति का ज्ञान करने के लिये हमें उसमें उपयुक्त संशोधन करने पड़ते हैं।
सिद्धान्त ज्योतिष – (ख) गतिशास्त्रीय ज्योतिष
गतिशास्त्रीय ज्योतिष में हम न्यूटन के व्यापक गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के प्रयोग द्वारा खगोलीय पिंडों की गतियों, कक्षाओं आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें हम सापेक्ष संशोधन कर देते हैं। इसका सफलतापूर्वक प्रयोग सौर परिवार, युग्म तारा, तथा बहुतारा पद्धतियों में हो चुका है।
सिद्धान्त ज्योतिष – (ग) भौतिक ज्योतिष
भौतिक ज्योतिष में हम आकाशीय पिंडों की भौतिक स्थितियों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके लिये हमारे मुख्य यंत्र वर्णक्रमदर्शी, प्रकाशमापी, तथा रेडियो दूरदर्शी हैं। वर्णक्रम विश्लेषण से हम आकाशीय पिंड के वायुमंडल, तापमान, मूलतत्व आदि का ज्ञान प्राप्त करते हैं।
सिद्धान्त ज्योतिष – आकाशीय पिण्ड
आकाशीय पिंडों को हम प्राय: तीन भागों में बाँटते हैं
(क) सूर्य तथा उसके परिवार के सदस्य
(ख) तारे
(ग) आकाशगंगाएँ
सिद्धान्त ज्योतिष – आकाशीय पिण्ड (१) सूर्य
सूर्य हमारा निकटतम तारा है। यह गैसों से बना गोला है, जिसका व्यास १३,९३,००० किलोमीटर है। इसका माध्य व्यास ३१°५९.३.०.१ है, यह सौर परिवार के केंद्र में है तथा इसकी द्रव्यमात्रा अत्यधिक होने के कारण यह अपने परिवार के सदस्यों की गतिविधि पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। इसकी पृथ्वी से दूरी नौ करोड़ तीस लाख मील के लगभग, अथवा (१.४९६० ± .०००३)´१०८, किलोमीटर के तुल्य है। इसे ज्योतिष इकाई कहते हैं तथा सौर परिवार की कक्षाओं की दूरियां प्रायः इसी इकाई में व्यक्त की जाती हैं। इसकी द्रव्यमात्रा (१.९९१ ± .००२) ´ १०३३, ग्राम है। इसका सामान्य अवस्था में घनत्व पानी के सापेक्ष १.४१० ± .००२ है। इसके धरातल का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का २७.८९ गुना है। इसके पृष्ठतल का ताप ६,००० सेंo, केंद्र का ताप लगभग २,००,००,००० सेंo तथा प्रकाशमंडल का लगभग ५,००० सेंo है। इसका फोटो दृष्ट कांतिमान- २६.७३ ± .०३ है। सूर्य के पृष्ठतल की चमक प्रति वर्ग इंच १५,००,००० कैंडल पावर है। इसका निरपेक्ष कांतिमान ४.८४ ± .०३ है। इसके घूर्णाक्ष का आनतिकोण ७°१५’ है। यह प्रति सेकंड (३.८६ ± ०३)१०३३ अर्ग ऊर्जा प्रसारित करता है। पलायन वेग पृथ्वी के पृष्ठतल पर ११ किलोमीटर प्रति सेकंड तथा सूर्य के पृष्ठ पर ६१८ किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के तल पर, अपेक्षाकृत धुँधली पृष्ठीभूमि पर, असंख्य प्रकाशकण से दिखलाई देते हैं, जो चावल के कणों सरीखें प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे बहुत उष्ण बादल हैं जो अपेक्षाकृत धुँधली पृष्ठभूमि पर उड़ा करते हैं। सूर्य के प्रकाश मंडल में दूरदर्शी से देखने पर बड़े बड़े काले रंग के धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकाशमंडल के कम ताप के स्थान हैं। इनका ताप लगभग ४,००० केo होता है। इन्हें सूर्यकलंक कहते हैं। इनके वेध से पता चलता है कि सूर्य पृथ्वी के सापेक्ष अपनी धुरी की २७.२५ दिन में परिक्रमा करता है। सूर्य की अपने अक्ष के सापेक्ष परिक्रमा का नक्षत्रकाल २५.३५ दिन है। सूर्यकलंकों के पास कुछ चमकते भाग भी दिखलाई देते हैं, इन्हें अतिभा कहते हैं। जहाँ सूर्यकलंक होते हैं वहाँ अतिभा अवश्य होते हैं। सूर्य का वायुमंडल उत्क्रमण परत से प्रारंभ होता है। इसे सूर्य के वास्तविक वायुमंडल का भाग समझना चाहिए। यह सैंकड़ों मील घना है तथा इसका ताप प्रकाशमंडल से कम है। इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम का आधिक्य है, न्यून मात्रा में सिलिकन, आक्सजीन तथा अन्य परिचित गैसें भी मिलेंगी। उत्क्रमण परतों के ऊपर वर्णमंडल है। यह पूर्ण ग्रहण के अवसर पर ही दिखलाई देता है। इसका विस्तार ६,००० मील तक है। इसमें कैल्सियम, हाइड्रोजन तथा हीलियम पाए जाते हैं। इसका विस्ता एकरूप नहीं है। वर्णमंडल में सूर्य की कुछ महत्वपूर्ण आकृतियाँ हैं जिनमें से एक उड़ती हुई आग की लपटें हैं, जिन्हें सौर ज्वाला कहते हैं। कभी कभी ये सूर्य के प्रकाशमंडल से हजारों मील ऊपर उठी दिखाई देती हैं। पूर्ण ग्रहण के अवसर पर जब सूर्य का बिंब चंद्रमा से पूर्णतया ढक जाता है तब वर्णमंडल से ऊपर अत्युज्वल शुभ्र प्रकाश का जो परिवेष दिखाई देता है उसे सूर्यकिरीट कहते हैं।
सिद्धान्त ज्योतिष – आकाशीय पिण्ड (२) सौर परिवार
जो खगोलीय पिंड सूर्य की परिक्रमा करते हैं वे सौर परिवार के सदस्य हैं। इनमें ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, घूमकेतु तथा उल्काएँ हैं।
वे खगोलीय लघु ठोस पिंड जो किसी तारे की, विशेषतया सूर्य की, परिक्रमा करते हैं ग्रह हैं। सौर परिवार के ग्रह हैं : बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु शनि, वारुणी तथा वरुण। इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल तथा यम छोटे हैं तथा गुरु, वारुणी और वरुण विशाल हैं। बुध तथा शुक्र की कक्षाएँ सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी की कक्षा के भीतर पड़ती है। अत: इन्हें अंतर्ग्रह कहते हैं। शेष बहिर्ग्रह हैं।
सिद्धान्त ज्योतिष – आकाशीय पिण्ड (३) ग्रहों की कक्षाएँ
ग्रह ऐसी दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में भ्रमण करते हैं, जिनकी एक नाभि में सूर्य है। दोनों नाभियों से परिधि तक जानेवाली सरल रेखा को दीर्घ अक्ष तथा दीर्घवृत्त के केंद्र से दीर्घ अक्ष पर लंब रेखा के परिधि पर्यंत भाग को लघु अक्ष कहते हैं। दीर्घवृत्त परिधि का वह बिंदु जो रवि के निकट दीर्घ अक्ष पर स्थित है उसे रविनीच, तथा जो बिंदु दीर्घ अक्ष के दूसरी ओर है उसे सूर्योच्च कहते हैं। दीर्घ अक्ष पर सूर्योच्च तथा रविनीच स्थिति हैं, इसलिये इसे नीचोच्च रेखा कहते हैं। रविनीच से नाभि स्थित सूर्य पर परिधि का कोण कोणिकांतर कहलाता है। ग्रह के रविनीच अथवा सूर्योच्च के सापेक्ष परिक्रमा काल को परिवर्ष कहते हैं। ग्रहों की कक्षाएँ क्रांतिवृत्त के धरातल में नहीं हैं, किंतु उससे झुकी हुई हैं। ग्रह की कक्षा तथा क्रांतिवृत्त के संपातबिंदु को पात कहते हैं। जहाँ से ग्रह क्रांतिवृत्त से ऊपर की ओर जाता है वह बिंदु अरोहपात कहलाता है तथा दूसरा आवरोहपात। आकाश में ग्रह की स्थिति जानने के लिये हमें ग्रह का दीर्घ अक्ष, उत्केंद्रता, कक्षा की क्रांतिवृत्त से नति, निर्देशक्षण, सूर्योच्च की स्थिति तथा पात की स्थिति का ज्ञान करना आवश्यक है। ग्रहों में घूर्णन तथा परिक्रमण की दो प्रकार की गतियाँ पाई जाती हैं। एक तो वे अपने कक्षा में चलते हुए सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसे उनका परिक्रमण कहते हैं। जब कोई ग्रह किसी तारे के सापेक्ष सूर्य की परिक्रमा करता है, तो उसे उसका नाक्षत्र काल कहते हैं। ग्रह के पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमण काल को संयुति काल कहते हैं।
सिद्धान्त ज्योतिष – आकाशीय पिण्ड, (४) ग्रहों की पृथ्वी के सापेक्ष गति
पृथ्वी के निवासियों को बहिर्ग्रह तो पृथ्वी की परिक्रमा करते दिखलाई देते हैं, किंतु अंतर्ग्रह सूर्य से पूर्व तथा पश्चिम दोलन करते दिखलाई देते हैं। यह उनकी कक्षाओं की विशेष स्थिति के कारण है। पृथ्वी के सापेक्ष अंतर्ग्रह की सूर्य से चरमकोणीय दूरी को चरम वितान कहते हैं। जब अंतर्ग्रह सूर्य तथा पृथ्वी को मिलानेवाली सरल रेखा में होता है तो उसे ग्रह की अंतर्युति तथा जब अंतर्ग्रह तथा पृथ्वी को मिलानेवाली सरल रेखा सूर्य के केंद्र से होकर जाती है तो उसे बहिर्युति कहते हैं। बहिर्ग्रह को पृथ्वी से मिलानेवाली रेखा जब सूर्य में से होकर जाती है, तो उसे संयुति तथा जब ग्रह पृथ्वी और सूर्य को मिलानेवाली रेखा के बीच में रहता है तो उसे ग्रह की वियुति कहते हैं। ग्रह की एक संयुति से दूसरी संयुति तक के समय को संयुतिकाल कहते हैं बहिर्ग्रहों का यही, पृथ्वी के सापेक्ष, राशिचक्र की परिक्रमा का काल होता है। अंतर्ग्रह प्राय: पृथ्वी की परिक्रमा काल में ही राशिचक्र की परिक्रमा करते हैं। अपनी कक्षाओं में गति की दिशा एक ही होने के कारण अंतर्ग्रह अंतर्युति के आसन्न तथा बहिर्ग्रह वियुति के आसन्न काल में पृथ्वी के सापेक्ष विरुद्ध दिशा में चलते प्रतीत होते हैं। इस कारण ये हमें राशिचक्र में पश्चिम की ओर जाते दिखलाई देते हैं। यह ग्रहों की वक्रगति है। ग्रहों की, वक्रगति प्राप्त करने के कुछ समय पूर्व, पृथ्वी के सापेक्ष गति स्थिर हो जाती है। इससे ग्रह स्थिर से प्रतीत होते हैं। अंतर्युति अथवा वियुति के समय में ग्रह की वक्र गति परमाधिक होती है1 उसके कुछ काल बाद यह कम होने लगती है, फिर ग्रह स्थिर प्रतीत होकर ऋजु गति से चलते लगता है।
सिद्धान्त ज्योतिष – आकाशीय पिण्ड, (५) ग्रहकलाएँ
अंतर्ग्रहों के प्रकाशित भाग चंद्रमा की तरह कम तथा अधिक प्रकाशित होते रहते हैं और ये कलाएँ प्राप्त करते हैं। इनके आकारों के अति छोटा होने के कारण बिना यंत्र के इनकी कलाएँ दिखलाई नहीं पड़तीं। बहिर्ग्रहों की कलाएँ सदा अर्धाधिक रहती है।
सिद्धान्त ज्योतिष – आकाशीय पिण्ड, (६) उपग्रह
जस प्रकार ग्रह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। व्यापक गुरुत्वाकर्षण नियम से यह स्पष्ट है कि इनकी द्रव्यमात्राएँ अपने ग्रहों से कम होती हैं। पृथ्वी के उपग्रह का चंद्रमा कहते हैं। चंद्रमा का हमारे जीवन से बहुत संबंध है। धार्मिक कृत्यों के लिये अभी बहुत से देशों में चांद्र मासों का व्यवहार किया जाता है। चंद्रमा को प्राचीन काल में ग्रह माना जाता था। पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल के दो, गुरु के १२, शनि के ९, वारुणी (यूरेनस) के ५, तथा वरुण (नेप्चून) के २ उपग्रह हैं। बुध, शुक्र तथा यम का कोई भी उपग्रह नहीं है
सिद्धान्त ज्योतिष – आकाशीय पिण्ड, (७) ग्रहण तथा ताराप्रच्छादन
जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो अमावस्या के दिन पृथ्वी पर दृश्य सूर्य का भाग उससे ढक जाता है। इसे सूर्यग्रहण कहते हैं। इसी प्रकार जब पूर्णिमा की रात में चंद्रमा पृथ्वी की छाया में प्रविष्ट होकर प्रकाशहीन हो जाता है तो उसे चंद्रग्रहण करते हैं। सूर्य तथा चंद्रमा के ग्रहण बहुत प्रसिद्ध हैं। सूर्य के ग्रहणों से सूर्य के वायुमंडल तथा किरीट की प्रकृति के अध्ययन में बहुत सहायता मिलती है। गुरु के उपग्रहों के ग्रहणों के अध्ययन से सर्वप्रथम प्रकाश के वेग को ज्ञात किया गया। चंद्रमा द्वारा ताराओं के ढके जाने को ताराप्रच्छादन कहते हैं।
सिद्धान्त ज्योतिष – आकाशीय पिण्ड, (८) क्षुद्र ग्रह
बोडे ने ग्रहों की सूर्य से दूरियाँ ज्यौतिषीय इकाई में ज्ञात करने के लिये निम्नलिखित नियम बताया था–
दू ०.४ + ०.३ ´ २ न, जहाँ न = – ¥, ०,१,२,३,४,……..इससे बुध की दूरी ०.४, शुक्र की दूरी = ०.७, पृथ्वी की दूरी –१.० तथा मंगल की दूरी १.६ प्राप्त हुई।
यहाँ तक तो प्राय: ठीक है, किंतु गुरु की दूरी इस नियम से ठीक नहीं बैठती। परंतु यदि हम बीच में किसी और ग्रह की कल्पना कर लें, तो शेष ग्रहों की दूरियाँ इस नियम से ठीक बैठ जाती हैं। इसलिये ज्योतिषियों ने मंगल तथा गुरु की कक्षा के बीच अन्य ग्रह की खोज शुरू की। इससे उन्हें बहुत से क्षुद्रग्रह मिले। सर्वप्रथम क्षुद्रग्रह सीटो का आविष्कार जनवरी, १,८०१ ईसवी में इटली के ज्योतिषी पियाज़ी ने किया था। सन् १,९५० में क्षुद्रग्रहों की संख्या १,६०० तक पहुँच गई थी। अनुमान है कि इनकी संख्या १,००,००० होगी।
सिद्धान्त ज्योतिष – आकाशीय पिण्ड, (९) धूमकेतु
ये अति न्यून घनत्ववाली द्रव्यमात्रा के बने आकाशीय पिंड हैं, जो सूर्य के समीप आने पर सूर्य से विपरीत दिशा में बहुत दूर तक पुच्छ जैसे अपने भाग को प्रकाशित करते हैं। इनके आकार को मुख्यतया दो भागों में बाँटा जाता है। गोलाकार घने प्रकाशित भाग को सिर तथा हलके प्रकाशित भाग को पुच्छ कहते हैं। सिर में इनका नाभिक होता है। ये सूर्य के नियंत्रण में शांकव मार्गों में जाते हैं। इनमें कुछ की कक्षाएँ परवलयाकार तथा अतिपरवलयाकार दिखलाई पड़ती हैं, जिससे प्रतीत होता है कि कदाचित् गुरु ने अपने आकर्षण के कारण इन्हें सौर परिवार का सदस्य बना लिया। बहुत से धूमकेतु दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में नियतकाल में परिक्रमण करते हैं। इनमें हैलि का धूमकेतु प्रसिद्ध है। धूमकेतुओं की गति पर गुरु का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसके कारण इनकी कक्षा बदल जाती है। प्राचीन काल में धूमकेतु का दिखाई पड़ना अनिष्ट का सूचक माना जाता था।
सिद्धान्त ज्योतिष – आकाशीय पिण्ड, (१०) उल्काएँ
बहुधा रात्रि के समय कुछ चमकीले पदार्थ पृथ्वी की ओर अतिवेग से आते दिखाई देते हैं। इन्हें तारा का टूटना या उल्कापात कहते हैं। उल्काएँ हमें तभी दिखलाई देती हैं जब ये अतिवेग से पृथ्वी के वायुमंडल में घुसती हैं। इनका वेग ११ से लेकर ६२ किलोमीटर प्रति सेकेंड तक रहता है। ये जब हमारे धरातल से १०० तथा १२० किलोमीटर की दूरी के भीतर होती हैं तो हमें प्रथम बार दिखलाई पड़ती हैं और ५० या ६० किलोमीटर की दूरी तक आने पर अदृश्य हो जाती हैं। वस्तुत: पृथ्वी के घने वायुमंडल में अतिवेग से घुसने पर इनके द्रव्य में आग उत्पन्न हो जाती है और ये जल जाती हैं। इनकी द्रव्यमात्रा अत्यल्प होती है। कभी कभी उल्काएँ जब पृथ्वी पर गिरती हैं तो बड़े बड़े गड्ढ़े बना देती हैं। यदि हमारा वायुमंडल हमारी रक्षा न करे, तो उल्कापात से पृथ्वी तथा हमारी बहुत हानि हो।
सिद्धान्त ज्योतिष – आकाशीय पिण्ड, (११) तारे
ये गरम गैसों से स्वयं प्रकाशित खगोलीय पिंड हैं, जो अपने द्रव्य को निजी गुरुत्वाकर्षण से संबद्ध रखते हैं। तारों के समूह एक विशेष आकृति धारण कर लेते हैं, इन्हें तारामंडल कहते हैं। क्रांतिवृत्त के क्षेत्र के तारामंडलों को राशि कहते हैं, जो मेष, वृष, मिथुन आदि १२ हैं। सर्पधर का कुछ भाग वृश्चिक तथा धनु राशियों के बीच में है। क्रांतिवृत्त तथा खगोलीय ध्रुव के बीच २१ तथा सर्पधर के शेष भाग और क्रांतिवृत्त तथा दक्षिणी खगोलीय ध्रुव के बीच ४७ तारामंडल हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में इनके कुछ नाम ग्रीक पुराण कथाओं पर आधारित हैं तथा कुछ के नाम अरबी के हैं। नक्षत्रों के अश्विनी, भरणी, मृगशिरा आदि के भारतीय नाम भी पुराण कथाओं से संबद्ध हैं। राशियों में तारें की चमक के क्रम को बताने के लिये ग्रीक वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है। जिस तारामंडल में तारों की संख्या वर्णमाला के अक्षरों से अधिक होती है, उनकी चमक के क्रम को अंकों द्वारा भी व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक कांतिमान अपने अगले कांतिमान से ढाई (२.५) गुना अधिक चमकीला होता है। कांतिमान जितना कम होगा उतना ही तारों की सापेक्ष चमक ढाई (२.५) गुणा बढ़ जाएगी। इस प्रकार १ से ६ तक कांतिमान के तारों की चमक का अनुपात १०० : ४० : १६ : ६.३ : २.५ : १ होगा। तारों के रंग से उनके ताप का ज्ञान होता है। बिना यंत्र के देखने से भी रंग का पता चल जाता है, किंतु सूक्ष्म ज्ञान के लिये रंगप्रभावी लेप वाली फोटोग्राफी की प्लेटों, फिल्मों तथा वर्णक्रमदर्शी फोटोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। केवल आँख से दृश्य तारों की संख्या लगभग ६,५०० है। इनमें लगभग २० तारे १ से १.५ कांतिमान के लगभग, ५० तारे द्वितीय, १५० तारे तृतीय, ५०० तारे चतुर्थ, १,५०० तारे पंचम तथा शेष तारे छठे कांतिमान के हैं। केवल आँख से, छठे कांतिमान से कम चमकीले तारे नहीं देखे जा सकते। २०० इंच व्यास के दूरदर्शी की सहायता से २३वें कांतिमान तक के तारे देखे जा सकते हैं। अब तक बड़े दूरदर्शियों द्वारा देखे गए हमारी आकाशगंगा के तारों की संख्या १,०११ है। तारों की गतियों को दो भागों में बाँट देते हैं। एक तो वह, जिससे हमारे देखने की दिशा में आगे पीछे हटते हैं, दूसरी वह, जिससे तारे अतिदूरवर्ती तारों के सापेक्ष किसी दिशा में हटते दिखाई देते हैं। प्रथम को त्रिज्यावेग तथा द्वितीय को निजी गति कहते हैं। दोनों वेगों का लब्धवेग तारा का वास्तविक वेग होता है। त्रिज्यावेग को वर्णक्रम की लाल रेखाओं के विचलन से डॉपलर के नियम द्वारा जाना जाता है, तथा निजी गति को कुछ वर्षों के अंतराल से लिए गए फोटोग्राफों द्वारा। तारों की निजी गति बहुत कम होती है। ज्योतिषी बर्नार्ड ने सबसे अधिक निजी गति वाले तारे की वार्षिक निजी गति १०.३ ज्ञात की है। तारों की दूरियाँ नापने के लिये वार्षिक लंबन का प्रयोग किया जाता है। पृथ्वी की कक्षा का व्यास यदि आधार मान लें और शीर्षबिंदु पर तारे को मानें तो शीर्ष बिंदु पर बना कोण द्विगुण वार्षिक लंबन होगा। इसके लिये एक तारे के, छह महीने के अंतर पर, दो वेध लेने पड़ते हैं। किसी भी तारे का वार्षिक लंबन १.०० से अधिक नहीं। जिस तारे का लंबन १.००हो वह हमसे पृथ्वी की कक्षा के अर्धव्यास के २,०६,२६५ गुना दूरी पर होता है। इस दूरी को एक पारसेक कहते हैं। तारों की दूनियाँ इतनी अधिक हैं कि उनके लिये पारसेक इकाई का काम देता है। तारों की दूरियाँ नापने के लिये प्रकाशवर्ष भी इकाई के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रकशवर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश अपनी गति (१,८६,००० मील प्रति सेकेंड) से एक वर्ष में तय करता है। यह ५८,६०,००,००,००,००० मील है तथा पारसेक का ०.३०७ है। अति समीप के नक्षत्रों का वार्षिक लंबन सूर्य के सापेक्ष निजी गति के ज्ञान द्वारा, युग्म तारों का गतिशास्त्र द्वारा तथा शेष का वर्णक्रमदर्शी विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है। तारों के आकार के अधार पर उनके अतिदानवाकार, दनवाकार, सामान्यक्रम तथा वामनाकार भेद किए जाते हैं। इनका आकार उत्तरोत्तर छोटा होता जाता है। नवतारा नवजात तारा होता है। वस्तुत: यह पहले से विद्यमान होता है, जिसमें विस्फोट हो चुका होता है। नवतारा की विशेषता यह है कि एकाएक अति प्रकाशित होकर विस्फुटित हो जाता है। कुछ तारों का प्रकाश नियत क्रम से बढ़ता घटता रहता है। इन्हें चल तारे कहते हैं। इनमें सिफियस चतुर्थ तथा आर आर लाइरा क्रम के तारे महत्वपूर्ण हैं। सिफियस चतुर्थ की श्रेणी के तारों को सिफीड कहते हैं। इनमें प्रकाश के उतार चढ़ाव का उनके काल से निश्चित संबंध रहता है। जहाँ ऐसे तारे पाए जाते हैं यहाँ इस संबंध से तारापुंज की दूरी ज्ञात करना सरल होता है। आर आर लाइरा तारे प्रायः समान ऊँचाई पर रहते हैं। इनसे आकाशगंगा प्रणाली की दूरी ज्ञात करने में सहायता मिली है। नक्षत्रों के तल का ताप ज्ञात करने के लिये ज्योतिर्मिति द्वारा वर्णज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार लाल रंग के तारों के तल का ताप २,०००॰ – ३,०००॰ के॰, नारंगी रंग के तारों का ३,०००॰ – ५०००॰के॰ और नीले रंग के तारों का १२,०००॰ – २०,०००॰ – ३०,०००॰ के॰ अथवा और ऊपर होता है। वस्तुत: रंगों का ठीक ज्ञान वर्णक्रमदर्शी विधि से होता है। इसीलिये ताप के लिये वर्णक्रमदर्शी के आधार पर तारों के भेद को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार तारों के वर्णदर्शी क्रम से ओ, बी, ए, एफ, जी, के एम, आर, एन, एस, भेद किए जाते हैं। इनके उपभेदों को व्यक्त करने के लिये अंग्रेजी वर्णमाला के ए से इ तक के लघु अक्षरों, अथवा शून्य से ९ तक के अंकों, का प्रयोग करते हैं। कुछ तारे जोड़ों में होते हैं। इनमें साथी तारे पर सामान्य गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रयोग करके उसके अकार, द्रव्यमात्रा आदि का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी वामनाकार तारे की द्रव्यमात्रा सूर्य की द्रव्यमात्रा के ०.१ से कम नहीं पाई गई। सूर्य की द्रव्यमात्रा से दसगुनी द्रव्यमात्रा वाले दानवाकार तारे भी इने गिने ही हैं। शेष की द्रव्यमात्रा इन दो सीमाओं के भीतर रहती है। तारों का घनत्व आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी कारण दानवाकार तारों का घनत्व कम होता है। ज्येष्ठा तारे का घनत्व, जिसका व्यास सूर्य के व्यास का ४८० गुना है और जिसकी द्रव्यमात्रा सूर्य के २० गुने से अधिक नहीं है, साधारण वायु के ०.०००१ के बराबर है। औसत तारों के मूल तत्वों में ७०% हाइड्रोजन, २८% हीलियम, १.५% कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नियोन और .५% लौह वर्ग के भारी तत्व होते हैं। तारों के केंद्र की भीषण गर्मी से हाइड्रोजन के अणु हीलियम के अणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं। इस आणविक प्रतिक्रिया में कुछ द्रव्यमात्रा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, जिससे तारों को असीम ऊर्जा प्राप्त होती रहती है। इसका ये प्रकाश के रूप में वितरण करते रहते हैं। इसी प्रक्रिया के आधार पर तारों की आयु का निर्णय किया जाता है। अत्यधिक प्रकाशमान तारों की औसत आयु १०६ वर्ष, सामान्य क्रम के तारों की १०१० से लेकर १०१३ वर्ष तक की होती है।
सिद्धान्त ज्योतिष – आकाशीय पिण्ड, (१२) हमारी आकाशगंगा
यह कृष्णपक्ष की किसी रात्रि में उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई, धुँधले चमकीले नक्षत्रों की एक चौड़ी मेखला सी दिखलाई देती है। आकाशगंगा का पूर्वार्ध हंस, धनु में से होता हुआ करीना तक फैला है और दूसरे अर्धांश की अपेक्षा, जो हंस, मृगशिरा तथा करीना या नौतल तक फैला है, अत्यधिक चमकीला है। आकाशगंगा धनु के समीप अधिकतम चौड़ी तथा अधिकतम चमकीली है।
आकाशगंगा की मेखला के बीच से खगोल का जो बृहद्वृत्त जाता है उसे आकाशगंगीय विषुद्वृत्त कहते हैं। ऐक्विला, अथवा गरुड़, नामक तारामंडल के समीप खगोलीय विषुवद्वृत्त से लगभग ६२॰ का कोण बनाता है। इसी बिंदु को हम आकाशगंगीय नियामकों का मूल बिंदु मानते हैं।
सिद्धान्त ज्योतिष – आकाशीय पिण्ड, (१३) आकृति
हमारी आकाशगंगा सर्पिल आकार की है। इसका नाभिक सूर्य से लगभग २,७०० प्रकाशवर्ष की दूरी पर धनु राशि में स्थित है। इसके आकाशगंगीय नियामक, भोगांक ३२८॰ तथा विक्षेप ०॰अथवा – २॰, हैं। सूर्य उसकी बाहरी भुजा में है। इसके विषुवद्वृत्त का व्यास लगभग १०,००,००० प्रकाशवर्ष है। इसके केंद्रीय भाग में तारों की संख्या बहुत अधिक है। ज्यों ज्यों केंद्र से दूर हटते जाते हैं, तारों की संख्या कम होती जाती है। आकाशगंगा में लगभग १०११ तारे होंगे। इसकी द्रव्यमात्रा सूर्य की द्रव्यमात्रा की १०११ है। अतिशक्तिशाली दूरदर्शी से देखने पर बहुत से खगोलीय पदार्थ, पर्याप्त भाग में, चमकदार छोटे छोटे प्रकाशकणों से प्रकाशित दिखलाई देते हैं। इनमें से कुछ हमारी आकाशगंगा की तरह स्वयं विश्वद्वीप हैं। इसलिये इनका अध्ययन करना भी आवश्यक है। इन पदार्थों को हम इन भागों मे बाँट सकते हैं, नीहारिकाएँ, तारागुच्छ, तारामेघ तथा आकाशगंगाएँ। नीहारिकाएँ गैस से बने मेघ होती हैं, जिनके अणु पास के किसी बहुत उष्ण तारे के प्रखर प्रकाश के कारण आयनीकृत होकर चमकने लगते हैं। ये प्रकाशित नीहारिकाएँ कहलाती हैं, जैसे मृगशिरा की नीहारिका। जिन गैस मेघों को किसी उष्ण नक्षत्र की ऊर्जा नहीं मिलती उनके अणु प्रकाशित नहीं हो पाते और वे अन्य तारों के प्रकाश के अवरोधक हो जाते हैं। पास के प्रकाशित भाग की अपेक्षा वे भाग अंधकारपूर्ण होते हैं। ऐसी काली आकृति को काली नीहारिका कहते हैं, जैसे अश्वसिर नीहारिक। प्रारंभ में नीहारिका शब्द का अर्थ अस्पष्ट था तथा बड़े दूरदर्शी से किसी भी धुँधले, या अधिक प्रकाशित क्षेत्र, को नीहारिका कह देते थे, जैसे देवयानी निहारिका। किंतु वह नीहारीका न होकर स्वयं आकाशगंगा है।
सिद्धान्त ज्योतिष – आकाशीय पिण्ड, (१४) तारागुच्छ
कुछ तारों के समूह यंत्र बिना देखने पर प्रकाश के धब्बे से प्रतीत होते हैं, जिनसे कुछ छोटे तारे तथा एकाध चमकीला तारा दिखलाई पड़ता है। दूरदर्शी यंत्र से देखने पर इनमें सैकड़ों तारे तथा एक दो नीहारिका जैसे पदार्थ भी दिखलाई देते हैं, जैसे कृत्तिका तारागुच्छ। तारागुच्छ के तारे प्राय: एक सी निजी गति से चलते दिखलाई देते हैं। तारागुच्छ दो प्रकार के होते हैं, आकाशगंगीय तारागुच्छ तथा गोलीय तारागुच्छ। कृत्तिका तारागुच्छ आकाशगंगीय तारागुच्छ है तथा बिना यंत्र के दिखलाई पड़ जाता है। एक आकाशगंगीय तारागुच्छ में कुछ सौ से लेकर कुछ हजार तक चमकीले तारे दिखलाई पड़ जाते हैं। आकाशगंगीय तारागुच्छ आकाशगंगा के धरातल में या उसके पास रहते हैं। चमकीले तारागुच्छ आकाशगंगा के धरातल से १०० से लेकर १,००० प्रकाशवर्षों तक की दूरी पर स्थित हैं, किंतु अधिकांश १,००० से १५,००० प्रकाश वर्षों की दूरी पर स्थित हैं। गोलीय तारागुच्छ आकाशगंगा के धरातल से दूर होते हैं। निकटतम गोलीय तारागुच्छ २०,००० प्रकाशवर्ष की दूरी पर होगा। इनमें हजारों तारे होते हैं, जो गोल के केंद्र के पास लगभग इस प्रकार इकट्ठे रहते हैं कि इन्हें बड़े दूरदर्शी से देखने पर भी उनकी आकृति स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़ती। गोलीय तारागुच्छ की आकृति लगभग गोलाकार रहती है, जिसका व्यास लगभग १०० प्रकाशवर्ष होता है। इनका घना केंद्रीय भाग ५ प्रकाशवर्षों के लगभग होता है।
सिद्धान्त ज्योतिष – आकाशीय पिण्ड, (१५) तारामेघ
खगोल में कहीं कहीं चमकीले भाग मेघाकार प्रतीत होते हैं। बड़े दूरदर्शी से देखने पर इनमें असंख्य तारे दिखलाई पड़ते हैं। इनमें से कुछ आकाशगंगाएँ हैं। दो तारामेघ प्रसिद्ध हैं। बड़ा मेगलानिक तारामेघ तथा छोटा मेगलानिक। मेघ वस्तुतः आकाशगंगाएँ हैं, जो हमारी अपनी आकाशगंगा के निकटतम हैं। अपनी आकाशगंगा के अध्ययन से हमें अन्य आकाशगंगाओं का पता चला है एवं हमारी कुछ गलत धारणाएँ भी दूर हुई हैं। प्रत्येक नीहारिका आकाशगंगा नहीं है, यद्यपि कुछ आकाशगंगाएँ ऐसी भी हैं जिन्हें हम नीहारिका समझे बैठे थे।
आकाशगंगाएँ कई प्रकार की होती है, सर्पिल, दीर्घवृत्ताकार तथा अनियमित। देवयानी आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा की ही भाँति सर्पिल आकार की है। आकाशगंगा के अध्ययन से हमें विश्व की सीमा तथा उसकी उत्पत्ति एवं विकास के ज्ञान में सहायता मिलती है। हमारे बड़े से बड़े दूरदर्शक भी विश्व की अंतिम सीमा तक नहीं पहुँच सके हैं, तथापि आकाशगंगा के त्रिज्यावेगों के अध्ययन से हमने इतना जान लिया है कि अभी विश्व का विस्तार हो रहा है। यह लेमित्रे तथा एडिंगटन का मत है। इसी सिद्धांत के आधार पर अनुमान है कि विश्व की उत्पत्ति कदाचित् १० वर्ष पूर्व हुई होगी।
हमारा ज्योतिष का वर्तमान ज्ञान भूतल पर लगे यंत्रों से प्राप्त हुआ है। इनकी अपनी सीमा है। इसीलिये हमारा ज्ञान भी सीमित है। पिछले कुछ वर्षों से विज्ञान में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। गुब्बारों पर दूरदर्शियों को बहुत ऊँचा भेजने का प्रयास किया जा रहा है। राँकेट तथा कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के वायुमंडल के अज्ञात तत्वों तथा सौर परिवार के सूक्ष्म पदार्थों के अध्ययन का साधन बन रहे हैं। बड़े बड़े रेडियों दूरदर्शी तथा राडार यंत्र ज्योतिष को नई दिशा दिखला रहे हैं। इससे यह आशा की जा रही है कि हमें निकट भविष्य में खगोल के बहुत से नवीन रहस्यों का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।
(३). फलित ज्योतिष
फलित ज्योतिष उस विद्या को कहते हैं जिसमें मनुष्य तथा पृथ्वी पर, ग्रहों और तारों के शुभ तथा अशुभ प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष शब्द का यौगिक अर्थ ग्रह तथा नक्षत्रों से संबंध रखनेवाली विद्या है। इस शब्द से यद्यपि गणित (सिद्धांत) ज्योतिष का भी बोध होता है, तथापि साधारण लोग ज्योतिष विद्या से फलित विद्या का अर्थ ही लेते हैं।
ग्रहों तथा तारों के रंग भिन्न-भिन्न प्रकार के दिखलाई पड़ते हैं, अतएव उनसे निकलनेवाली किरणों के भी भिन्न भिन्न प्रभाव हैं। इन्हीं किरणों के प्रभाव का भारत, बैबीलोनिया, खल्डिया, यूनान, मिस्र तथा चीन आदि देशों के विद्वानों ने प्राचीन काल से अध्ययन करके ग्रहों तथा तारों का स्वभाव ज्ञात किया। पृथ्वी सौर मंडल का एक ग्रह है। अतएव इसपर तथा इसके निवासियों पर मुख्यतया सूर्य तथा सौर मंडल के ग्रहों और चंद्रमा का ही विशेष प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी विशेष कक्षा में चलती है जिसे क्रांतिवृत्त कहते हैं। पृथ्वी फलित ज्योतिष उस विद्या को कहते हैं जिसमें मनुष्य तथा पृथ्वी पर, ग्रहों और तारों के शुभ तथा अशुभ प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। ज्योतिष शब्द का यौगिक अर्थ ग्रह तथा नक्षत्रों से संबंध रखनेवाली विद्या है। इस शब्द से यद्यपि गणित (सिद्धांत) ज्योतिष का निवासियों को सूर्य इसी में चलता दिखलाई पड़ता है। इस कक्षा के इर्द गिर्द कुछ तारामंडल हैं, जिन्हें राशियाँ कहते हैं। इनकी संख्या है। मेष राशि का प्रारंभ विषुवत् तथा क्रांतिवृत्त के संपातबिंदु से होता है। अयन की गति के कारण यह बिंदु स्थिर नहीं है। पाश्चात्य ज्योतिष में विषुवत् तथा क्रातिवृत्त के वर्तमान संपात को आरंभबिंदु मानकर, ३०-३० अंश की १२ राशियों की कल्पना की जाती है। भारतीय ज्योतिष में सूर्यसिद्धांत आदि ग्रंथों से आनेवाले संपात बिंदु ही मेष आदि की गणना की जाती है। इस प्रकार पाश्चात्य गणनाप्रणाली तथा भारतीय गणनाप्रणाली में लगभग २३ अंशों का अंतर पड़ जाता है। भारतीय प्रणाली निरयण प्रणाली है। फलित के विद्वानों का मत है कि इससे फलित में अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि इस विद्या के लिये विभिन्न देशों के विद्वानों ने ग्रहों तथा तारों के प्रभावों का अध्ययन अपनी अपनी गणनाप्रणाली से किया है। भारत में १२ राशियों के २७ विभाग किए गए हैं, जिन्हें नक्षत्र कहते हैं। ये हैं अश्विनी, भरणी आदि। फल के विचार के लिये चंद्रमा के नक्षत्र का विशेष उपयोग किया जाता है।
ज्योतिषशास्त्र (ग्रीक भाषा ἄστρον के शब्द एस्ट्रोन, अर्थात “तारा समूह” -λογία और लॉजिया ( logia), यानि “अध्य्यन” से लिया गया है). यह प्रणालियों, प्रथाओं और मतों का वो समूह है जिसके ज़रिये आकाशीय पिंडो (celestial bodies) की तुलनात्मक स्थिति और अन्य सम्बंधित विवरणों के आधार पर व्यक्तित्व, मनुष्य की ज़िन्दगी से जुड़े मामलों और अन्य सांसारिक विषयों को समझकर, उनकी व्याख्या की जाती है और इस सन्दर्भ में सूचनाएं संगठित की जाती हैं। ज्योतिष जाननेवाले को ज्योतिषी या एक भविष्यवक्ता कहा जाता है। तीसरी सहस्राब्दी ई.पू. में इसके प्राचीनतम अभिलिखित लेखों से अब तक, ज्योतिष के सिद्धांतों के आधार पर कई प्रथाओं और अनुप्रयोगों के निष्पादन हुआ है। संस्कृति, शुरूआती खगोल विज्ञान और अन्य विद्याओं को आकार देने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
आधुनिक युग से पहले ज्योतिष और खगोल विज्ञान अक्सर अविभेद्य माने जाते थे। भविष्य के बारे में जानना और दैवीय ज्ञान की प्राप्ति, खगोलीय अवलोकन के प्राथमिक प्रेरकों में से एक हैं।पुनर्जागरण से लेकर १८ वीं सदी के अंत के बाद से खगोल विज्ञान का धीरे धीरे विच्छेद होना शुरू हुआ। फलतः खगोल विज्ञान ने खगोलीय वस्तुओं के वैज्ञानिक अध्ययन और एक ऐसे सिद्धांत के रूप में अपनी एक पहचान बनाई जिसका उसकी ज्योतिषीय समझ से कुछ लेना देना नहीं था।
ज्योतिषों का विश्वास है की खगोलीय पिंडों की चाल और उनकी स्थिति या तो पृथ्वी को सीधे तरीके से प्रभावित करती है या फिर किसी प्रकार से मानवीय पैमाने पर या मानव द्वारा अनुभव की जाने वाली घटनाओं से सम्बद्ध होती है। आधुनिक ज्योतिषियों द्वारा ज्योतिष को एक प्रतीकात्मक भाषा एक कला के रूप में या भविष्यकथन के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि बहुत से वैज्ञानिकों ने इसे एक छद्म विज्ञान या अंधविश्वास का नाम दिया है। परिभाषाओं में अन्तर के बावजूद, ज्योतिष विद्या की एक सामान्य धारणा यह है की खगोलीय पिण्ड अपने क्रम स्थान से भूत और वर्तमान की घटनाओं और भविष्यवाणी को समझने में मदद कर सकते हैं। एक मतदान में, ३१% अमिरिकियों ने ज्योतिष पर अपना विश्वास प्रकट किया और एक अन्य अध्ययन के अनुसार, ३९% ने उसे वैज्ञानिक माना है।
फलित ज्योतिष वैज्ञानिक आधार
ज्योतिष के आधार पर शुभाशुभ फल ग्रहनक्षत्रों की स्थितिविशेष से बतलाया जाता है। इसके लिये हमें सूत्रों से गणित द्वारा ग्रह तथा तारों की स्थिति ज्ञात करनी पड़ती है, अथवा पंचांगों, या नाविक पंचागों, से उसे ज्ञात किया जाता है। ग्रह तथा नक्षत्रों की स्थिति प्रति क्षण परिवर्तनशील है, अतएव प्रति क्षण में होनेवाली घटनाओं पर ग्रह तथा नक्षत्रों का प्रभाव भी विभिन्न प्रकार का पड़ता है। वास्तविक ग्रहस्थिति ज्ञात करने के लिए गणित ज्योतिष ही हमारा सहायक है। यह फलित ज्योतिष के लिये वैज्ञानिक आधार बन जाता है।
फलित ज्योतिष → (कुंडली)
कुंडली वह चक्र है, जिसके द्वारा किसी इष्ट काल में राशिचक्र की स्थिति का ज्ञान होता है। राशिचक्र क्रांतिचक्र से संबद्ध है, जिसकी स्थिति अक्षांशों की भिन्नता के कारण विभिन्न देशों में एक सी नहीं है। अतएव राशिचक्र की स्थिति जानने के लिये स्थानीय समय तथा अपने स्थान में होनेवाले राशियों के उदय की स्थिति (स्वोदय) का ज्ञान आवश्यक है। हमारी घड़ियाँ किसी एक निश्चित याम्योत्तर के मध्यम सूर्य के समय को बतलाती है। इससे सारणियों की, जो पंचागों में दी रहती हैं, सहायता से हमें स्थानीय स्पष्टकाल ज्ञात करना होता है। स्थानीय स्पष्टकाल को इष्टकाल कहते हैं। इष्टकाल में जो राशि पूर्व क्षितिज में होती है उसे लग्न कहते हैं। तात्कालिक स्पष्ट सूर्य के ज्ञान से एवं स्थानीय राशियों के उदयकाल के ज्ञान से लग्न जाना जाता है। इस प्रकार राशिचक्र की स्थिति ज्ञात हो जाती है। भारतीय प्रणाली में लग्न भी निरयण लिया जाता है। पाश्चात्य प्रणाली में लग्न सायन लिया जाता है। इसके अतिरिक्त वे लोग राशिचक्र शिरोबिंदु (दशम लग्न) को भी ज्ञात करते हैं। भारतीय प्रणाली में लग्न जिस राशि में होता है उसे ऊपर की ओर लिखकर शेष राशियों को वामावर्त से लिख देते हैं। लग्न को प्रथम भाव तथा उसके बाद की राशि को दूसरे भाव इत्यादि के रूप में कल्पित करते हैं1 भावों की संख्या उनकी कुंडली में स्थिति से ज्ञात होती है। राशियों का अंकों द्वारा तथा ग्रहों को उनके आद्यक्षरों से व्यक्त कर देते हैं। इस प्रकर का राशिचक्र कुंडली कहलाता है। भारतीय पद्धति में जो सात ग्रह माने जाते हैं, वे हैं सूर्य, चंद्र, मंगल आदि। इसके अतिरिक्त दो तमो ग्रह भी हैं, जिन्हें राहु तथा केतु कहते हैं। राहु को सदा क्रांतिवृत्त तथा चंद्रकक्षा के आरोहपात पर तथा केतु का अवरोहपात पर स्थित मानते हैं। ये जिस भाव, या जिस भाव के स्वामी, के साथ स्थित हों उनके अनुसार इनका फल बदल जाता है। स्वभावत: तमोग्रह होने के कारण इनका फल अशुभ होता है। पाश्चात्य प्रणाली में (१) मेष, (२) वृष, (३) मिथुन, (४) कर्क, (५) सिंह, (६) कन्या, (७) तुला, (८) वृश्चिक, (९) धनु, (१०) मकर, (११) कुंभ तथा (१२) मीन राशियों के लिये क्रमश: निम्नलिखित चिह्न हैं : १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२
(१) बुध, (२) शुक्र, (३) पृथ्वी, (४) मंगल, (५) गुरु, (६) शनि, (७) वारुणी, (८) वरुण, तथा (९) यम ग्रहों के लिये क्रमश: निम्नलिखित चिह्न : १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९
तथा सूर्य के लिये और चंद्रमा के लिये प्रयुक्त होते हैं।
भावों की स्थिति अंकों से व्यक्त की जाती है। स्पष्ट लग्न को पूर्वबिंदु (वृत्त को आधा करनेवाली रेखा के बाएँ छोर पर) लिखकर, वहाँ से वृत्त चतुर्थांश के तुल्य तीन भाग करके भावों को लिखते हैं। ग्रह जिन राशियों में हो उन राशियों में लिख देते हैं। इस प्रकार कुंडली बन जाती है, जिसे अंग्रेजी में हॉरोस्कोप (horoscope) कहते हैं। यूरोप में, भारतीय सात ग्रहों के अतिरिक्त, वारुणी, वरुण तथा यम के प्रभाव का भी अध्ययन करते हैं।
फलित ज्योतिष → (फल का ज्ञान)
फल के ज्ञान के लिये राशियों के स्वभाव का अध्ययन करना पड़ता है। कुंडली के विभिन्न भावों से हमारे जीवन से संबंध रखनेवाली विभिन्न बातों का पता चलता है, जैसे प्रथम भाव से शरीर संबंधी, दूसरे भाव से धन संबंधी आदि।
फलित ज्योतिष → (ग्रहदशा)
ग्रहों का विशेष फल देने का समय तथा अवधि भी निश्चित है। चंद्रनक्षेत्र का व्यतीत तथा संपूर्ण भोग्यकाल ज्ञात होने से ग्रहदशा ज्ञात हो जाती है। ग्रह अपने शुभाशुभ प्रभाव विशेष रूप से अपनी दशा में ही डालते हैं। किसी ग्रह की दशा में अन्य ग्रह भी अपना प्रभाव दिखलाते हैं। इसे उन ग्रहों की अंतर्दशा कहते हैं। इसी प्रकार ग्रहों की अंतर, प्रत्यंतर दशाएँ भी होती है। ग्रहों की पारस्परिक स्थिति से एक योग बन जाता है जिसका विशेष फल होता है। वह फल किस समय प्राप्त होगा, इसका निर्णय ग्रहों की दशा से ही किया जा सकता है। भारतीय प्रणाली में विंशोत्तरी महादशा का मुख्यतया प्रयोग होता है। इसके अनुसार प्रत्येक मनुष्य की आयु १२० वर्ष की मानकर ग्रहों का प्रभाव बताया जाता है।
फलित ज्योतिष → (शाखाएँ)
फलित ज्योतिष की कई शाखाएँ हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में इनकी संख्या छह है:
- (१) व्यक्तियों तथा वस्तुओं के जीवन संबंधी ज्योतिष
- (२) प्रश्न ज्योतिष,
- (३) राष्ट्र तथा विश्व संबंधी ज्योतिष,
- (४) वायुमंडल संबंधी ज्योतिष,
- (५) आयुर्वेद ज्योतिष तथा
- (६) ज्योतिषदर्शन।
भारतीय ज्योतिष में केवल जातक तथा संहितास दो शाखाएँ ही मुख्य हैं। पाश्चात्य ज्योतिष की (१), (२) तथा (३) शाखाओं का जातक में तथा शेष तीन का संहिता ज्योतिष में अंतर्भाव हो जाता है।
फलित ज्योतिष → (घटक) ग्रह
सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिण्डों को ग्रह कहते हैं।
- सूर्य Sun (पुल्लिंग) विंशोत्तरी दशा ६ वर्ष
- चंद्र Moon (स्त्रीलिंग) विंशोत्तरी दशा १० वर्ष
- मंगल Mars (पुल्लिंग) विंशोत्तरी दशा ७ वर्ष
- बुध Mercury (नपुंसक) विंशोत्तरी दशा १७ वर्ष
- बृहस्पति Jupiter (पुल्लिंग) विंशोत्तरी दशा १६ वर्ष
- शुक्र Venus (स्त्रीलिंग) विंशोत्तरी दशा २० वर्ष
- शनि Saturn (पुल्लिंग) विंशोत्तरी दशा १९ वर्ष
- राहु Dragon’s Head (पुल्लिंग) विंशोत्तरी दशा १८ वर्ष
- केतु Dragon’s Tail (पुल्लिंग) विंशोत्तरी दशा १७ वर्ष
- (राहू एवं केतु वास्तविक गृह नहीं है इन्हे छायाग्रह मना गया है।)
ग्रहों कि आपसी मित्रता-शत्रुता और समानता इस प्रकार है :-
- सूर्य – मित्र ग्रह (चंद्र, मंगल, गुरु) शत्रु ग्रह (शुक्र, शनि) सम ग्रह (बुध)
- चंद्र – मित्र ग्रह (सूर्य) सम ग्रह (मंगल, गुरु, शुक्र, शनि,चंद्र,राहु, केतु)
- मंगल – मित्र ग्रह (सूर्य, चंद्र, गुरु) शत्रु ग्रह (बुध) सम ग्रह (शुक्र, शनि)
- बुध – मित्र ग्रह (सूर्य, शुक्र) सम ग्रह (मंगल, गुरु, शनि, चंद्र)
- गुरु – मित्र ग्रह (सूर्य, चंद्र, मंगल) शत्रु ग्रह (बुध, शुक्र) सम ग्रह (शनि)
- शुक्र – मित्र ग्रह (बुध, शनि) शत्रु ग्रह (सूर्य, चंद्र, मंगल) सम ग्रह (गुरु)
- शनि – मित्र ग्रह (बुध, शुक्र) शत्रु ग्रह (सूर्य, चंद्र) सम ग्रह (मंगल, गुरु)
फलित ज्योतिष → (घटक) राशि
राशिचक्र वह तारामण्डलों का चक्र है जो क्रान्तिवृत्त (एक्लिप्टिक) में आते है, यानि उस मार्ग पर आते हैं जो सूरज एक साल में खगोलीय गोले में लेता है। ज्योतिषी में इस मार्ग को बाराह बराबर के हिस्सों में बाँट दिया जाता है जिन्हें राशियाँ कहा जाता है। हर राशि का नाम उस तारामण्डल पर डाला जाता है जिसमें सूरज उस माह में (रोज दोपहर के बारह बजे) मौजूद होता है। हर वर्ष में सूरज इन बाराहों राशियों का दौरा पूरा करके फिर शुरू से आरम्भ करता है।
राशियाँ, राशिचक्र के उन बारह बराबर भागों को कहा जाता है जिन पर ज्योतिषी आधारित है। हर राशि सूरज के क्रांतिवृत्त पर आने वाले एक तारामंडल से सम्बन्ध रखती है और उन दोनों का एक ही नाम होता है, जैसे की मिथुन राशि और मिथुन तारामंडल। यह बारह राशियां हैं – (१)मेष राशि, (२) वृष राशि (३) मिथुन राशि, (४) कर्क राशि (५) सिंह राशि (६) कन्या राशि (७) तुला राशि (८) वॄश्चिक राशि (९) धनु राशि (१०) मकर राशि (११) कुम्भ राशि (१२) मीन राशि , इन बारह तारा समूह ज्योतिष के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं। यदि पृथ्वी, सूरज के केन्द्र और पृथ्वी की परिक्रमा के तल को चारो तरफ ब्रम्हाण्ड में फैलायें, तो यह ब्रम्हाण्ड में एक तरह की पेटी सी बना लेगा। इस पेटी को हम १२ बराबर भागों में बांटें तो हम देखेंगे कि इन १२ भागों में कोई न कोई तारा समूह आता है। हमारी पृथ्वी और ग्रह, सूरज के चारों तरफ घूमते हैं या इसको इस तरह से कहें कि सूरज और सारे ग्रह पृथ्वी के सापेक्ष इन १२ तारा समूहों से गुजरते हैं। यह किसी अन्य तारा समूह के साथ नहीं होता है इसलिये यह १२ महत्वपूर्ण हो गये हैं। इस तारा समूह को हमारे पूर्वजों ने कोई न कोई आकृति दे दी और इन्हे राशियां कहा जाने लगा।
यदि ३६०° को १२ से विभाजित किया जाए तो एक राशि ३०° की होती है।
- मेष (Aries) – चर स्वभाव, मंगल स्वामी
- वृषभ (Taurus) – स्थिर स्वभाव, शुक्र स्वामी
- मिथुन (Gemini) – द्विस्वभाव, बुध स्वामी
- कर्क (Cancer) – चर स्वभाव, चंद्र स्वामी
- सिंह (Leo) – स्थिर स्वभाव, सूर्य स्वामी
- कन्या (Virgo) – द्विस्वभाव, बुध स्वामी
- तुला (Libra) – चर स्वभाव, शुक्र स्वामी
- वृश्चिक (Scorpio) – स्थिर स्वभाव, मंगल स्वामी
- धनु (Sagittarius) – द्विस्वभाव, गुरु स्वामी
- मकर (Capricorn) – चर स्वभाव, शनि स्वामी
- कुम्भ (Aquarius) – स्थिर स्वभाव, शनि स्वामी
- मीन (Pisces) – द्विस्वभाव, गुरु स्वामी
फलित ज्योतिष → (घटक) नक्षत्र
आकाश में तारा-समूह को नक्षत्र कहते हैं। साधारणतः यह चन्द्रमा के पथ से जुड़े हैं, पर वास्तव में किसी भी तारा-समूह को नक्षत्र कहना उचित है। ऋग्वेद में एक स्थान पर सूर्य को भी नक्षत्र कहा गया है। अन्य नक्षत्रों में सप्तर्षि और अगस्त्य हैं।
नक्षत्र सूची अथर्ववेद, तैत्तिरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण और लगध के वेदांग ज्योतिष में मिलती है। भागवत पुराण के अनुसार ये नक्षत्रों की अधिष्ठात्री देवियाँ प्रचेतापुत्र दक्ष की पुत्रियाँ तथा चन्द्रमा की पत्नियाँ हैं।
तारे हमारे सौर जगत् के भीतर नहीं है। ये सूर्य से बहुत दूर हैं और सूर्य की परिक्रमा न करने के कारण स्थिर जान पड़ते हैं अर्थात् एक तारा दूसरे तारे से जिस ओर और जितनी दूर आज देखा जायगा उसी ओर और उतनी ही दूर पर सदा देखा जायगा। इस प्रकार ऐसे दो चार पास-पास रहनेवाले तारों की परस्पर स्थिति का ध्यान एक बार कर लेने से हम उन सबको दूसरी बार देखने से पहचान सकते हैं। पहचान के लिये यदि हम उन सब तारों के मिलने से जो आकार बने उसे निर्दिष्ट करके समूचे तारकपुंज का कोई नाम रख लें तो और भी सुभीता होगा। नक्षत्रों का विभाग इसीलिये और इसी प्रकार किया गया है।
चंद्रमा २७-२८ दिनों में पृथ्वी के चारों ओर घूम आता है। खगोल में यह भ्रमणपथ इन्हीं तारों के बीच से होकर गया हुआ जान पड़ता है। इसी पथ में पड़नेवाले तारों के अलग अलग दल बाँधकर एक एक तारकपुंज का नाम नक्षत्र रखा गया है। इस रीति से सारा पथ इन २७ नक्षत्रों में विभक्त होकर ‘नक्षत्र चक्र’ कहलाता है।
यदि ३६०° को २७ से विभाजित किया जाए तो एक नक्षत्र १३°२०’ (तेरह डिग्री बीस मिनट) का होता है, अर्थात एक राशि मे सवा-दो (२.२५) नक्षत्र होते है।
- १. अश्विनी – स्थिति {०- १३°२०’ मेष} नक्षत्र स्वामी (केतु) पद (चु चे चो ला), तारासंख्या (३), आकृति (घोड़ा)
- २. भरिणी – स्थिति {१३°२०’ – २६°४०’ मेष} नक्षत्र स्वामी (शुक्र) पद (ली लू ले पो), तारासंख्या (३), आकृति (त्रिकोण)
- ३. कृत्तिका – स्थिति {२६°४०’ मेष – १०°००’ वृषभ} नक्षत्र स्वामी (सूर्य) पद (अ ई उ ए), तारासंख्या (६), आकृति (अग्निशिखा)
- ४. रोहिणी – स्थिति {१० °००’ – २३°२०’ वृषभ}नक्षत्र स्वामी चंद्र (ओ वा वी वु), तारासंख्या (५), आकृति (गाड़ी)
- ५. म्रृगशिरा – स्थिति {२३°२०’ वृषभ – ६°४०’ मिथुन} नक्षत्र स्वामी (मंगल) पद (वे वो का की), तारासंख्या (३), आकृति (हरिणमस्तक वा विडालपद)
- ६. आर्द्रा – स्थिति {६°४०’ – २०°००’ मिथुन} नक्षत्र स्वामी (राहू) पद (कु घ ङ छ), तारासंख्या (१), आकृति (उज्वल)
- ७. पुनर्वसु – स्थिति {२०°००’ मिथुन- ३°२०’ कर्क} नक्षत्र स्वामी (गुरु) पद (के को हा ही), तारासंख्या (५ या ६), आकृति (धनुष या धर)
- ८. पुष्य – स्थिति {३°२०’ – १६°२०’ कर्क } नक्षत्र स्वामी (शनि) पद (हु हे हो ड), तारासंख्या (१ व ३), आकृति (माणिक्य वर्ण)
- ९. आश्लेषा – स्थिति {१६°४०’ कर्क- ०°००’ सिंह} नक्षत्र स्वामी (बुध) पद (डी डू डे डो), तारासंख्या (५), आकृति (कुत्ते की पूँछ या कुलाशचक्र)
- १०. मघा – स्थिति {०°००’ – १३°२०’ सिंह} नक्षत्र स्वामी (केतु) पद (मा मी मू मे), तारासंख्या (५), आकृति (हल)
- ११. पूर्वा फाल्गुनी – स्थिति {१३°२०’ – २६°४०’ सिंह} नक्षत्र स्वामी (शुक्र) पद (नो टा टी टू), तारासंख्या (२), आकृति (खट्वाकार × उत्तर दक्षिण)
- १२. उत्तराफाल्गुनी – स्थिति {२६°४०’ सिंह- १०°००’ कन्या} नक्षत्र स्वामी (सूर्य) पद (टे टो पा पी), तारासंख्या (२), आकृति (शय्याकार × उत्तर दक्षिण)
- १३. हस्त – स्थिति {१०°००’ – २३°२०’ कन्या} नक्षत्र स्वामी (चंद्र) पद (पू ष ण ठ), तारासंख्या (५), आकृति (हाथ का पंजा)
- १४. चित्रा – स्थिति {२३°२०’ कन्या- ६°४०’ तुला} नक्षत्र स्वामी(मंगल) पद (पे पो रा री), तारासंख्या (१), आकृति (मुक्तावत् उज्वल)
- १५. स्वाति – स्थिति {६°४०’ – २०°०० तुला} नक्षत्र स्वामी(राहू) पद( रू रे रो ता), तारासंख्या (१), आकृति (कुंकुंवर्ण)
- १६. विशाखा – स्थिति {२०°००’ तुला- ३°२०’ वृश्चिक} नक्षत्र स्वामी(गुरु) पद (ती तू ते तो), तारासंख्या (५ व ६), आकृति (तोरण व माला)
- १७. अनुराधा – स्थिति {३°२०’ – १६°४०’ वृश्चिक} नक्षत्र स्वामी(शनि) पद (ना नी नू ने), तारासंख्या (७), आकृति (सूप या जलधारा)
- १८. ज्येष्ठा – स्थिति {१६°४०’ वृश्चिक – ०°००’ धनु} नक्षत्र स्वामी( बुध) पद (नो या यी यू), तारासंख्या (३), आकृति (सर्प या कुंडल)
- १९. मूल – स्थिति {०°००’ – १३°२०’ धनु} नक्षत्र स्वामी (केतु) पद (ये यो भा भी), तारासंख्या (९ या ११), आकृति (शंख या सिंह की पूँछ)
- २०. पूर्वाषाढ़ा – स्थिति {१३°२०’ – २६°४०’ धनु} नक्षत्र स्वामी (शुक्र) पद (भू धा फा ढा), तारासंख्या (४), आकृति (सूप या हाथी दाँत)
- २१. उत्तराषाढ़ा – स्थिति {२६°४०’ धनु- १०°००’ मकर} नक्षत्र स्वामी( सूर्य) पद (भे भो जा जी), तारासंख्या (४), आकृति (सूप)
- २२. श्रवण – स्थिति { १०°००’ – २३°२०’ मकर} नक्षत्र स्वामी(चंद्र) पद (खी खू खे खो), तारासंख्या (३), आकृति (बाण या त्रिशूल)
- २३. धनिष्ठा – स्थिति {२३°२०’ मकर- ६°४०’ कुम्भ} नक्षत्र स्वामी (मंगल) पद (गा गी गु गे), तारासंख्या (५), आकृति (मर्दल बाजा)
- २४. शतभिषा – स्थिति {६°४०’ – २०°००’ कुम्भ} नक्षत्र स्वामी (राहू) पद (गो सा सी सू), तारासंख्या (१००), आकृति (मंडलाकार)
- २५. पूर्वाभाद्रपदा – स्थिति {२०°००’ कुम्भ – ३°२०’ मीन} नक्षत्र स्वामी (गुरु) पद (से सो दा दी), तारासंख्या (२), आकृति (भारवत् या घंण्टाकार)
- २६. उत्तराभाद्रपदा – स्थिति {३°२०’ – १६°४०’ मीन } नक्षत्र स्वामी (शनि) पद (दू थ झ ञ), तारासंख्या (२), आकृति (दो मस्तक)
- २७. रेवती – स्थिति {१६°४०’ – ३०°००’ मीन} नक्षत्र स्वामी (बुध) पद (दे दो च ची), तारासंख्या (३२), आकृति (मछली या मृदंङ्ग)
इन २७ नक्षत्रों के अतिरिक्त ‘अभिजित्‘ नाम का एक और नक्षत्र पहले माना जाता था पर वह पूर्वाषाढ़ा के भीतर ही आ जाता है, इससे अब २७ ही नक्षत्र गिने जाते हैं। इन्हीं नक्षत्रों के नाम पर महीनों के नाम रखे गए हैं। महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा जिस नक्षत्र पर रहेगा उस महीने का नाम उसी नक्षत्र के अनुसार होगा, जैसे कार्तिक की पूर्णिमा को चंद्रमा कृत्तिका वा रोहिणी नक्षत्र पर रहेगा, अग्रहायण की पूर्णिमा को मृगशिरा वा आर्दा पर; इसी प्रकार और समझिए।
फलित ज्योतिष → परंपरायें
ज्योतिषियों की बहुत सारी परमपराएँ हैं, जिनमें से कुछ ज्योतिष सिद्धांतों और संस्कृतियों के प्रसारण के कारण एक सी विशेषता वाली होती हैं अन्य दूसरी परंपराओं का विकास विलगन में हुआ और उनके ज्योतिष सिद्धांत अलग हैं, हालांकि उनमें भी एक ही खगोलीय स्रोत से लिए जाने के कारण कुछ सामान्य विशेषताएं होती हैं।
फलित ज्योतिष → (परंपरायें) १ वर्तमान परंपराएँ
आधुनिक ज्योतिषियों द्वारा जिन मुख्य परम्पराओं का इस्तेमाल किया जाता है, वो हैं: १ वैदिक ज्योतिष २ पश्चिमी ज्योतिष ३ चीनी ज्योतिष
फलित ज्योतिष → (परंपरायें) (वर्तमान परंपराएँ) १. वैदिक ज्योतिष >>
वेद से जन्म लेने के कारण इसे वैदिक ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। वैदिक ज्योतिष को परिभाषित किया जाए तो कहेंगे कि वैदिक ज्योतिष ऐसा विज्ञान या शास्त्र है जो आकाश मंडल में विचरने वाले ग्रहों जैसे सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध के साथ राशियों एवं नक्षत्रों का अध्ययन करता है और इन आकाशीय तत्वों से पृथ्वी एवं पृथ्वी पर रहने वाले लोग किस प्रकार प्रभावित होते हैं उनका विश्लेषण करता है। वैदिक ज्योतिष में गणना के क्रम में राशिचक्र, नवग्रह, जन्म राशि को महत्वपूर्ण तत्व के रूप में देखा जाता है।
(क) राशि और राशिचक्र : राशि और राशिचक्र को समझने के लिए नक्षत्रों को को समझना आवश्यक है क्योकि राशि नक्षत्रों से ही निर्मित होते हैं। वैदिक ज्योतिष में राशि और राशिचक्र निर्धारण के लिए ३६० डिग्री का एक आभाषीय पथ निर्धारित किया गया है। इस पथ में आने वाले तारा समूहों को २७ भागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक तारा समूह नक्षत्र कहलाते हैं। नक्षत्रो की कुल संख्या २७ है। २७ नक्षत्रों को ३६० डिग्री के आभाषीय पथ पर विभाजित करने से प्रत्येक भाग १३ डिग्री २० मिनट का होता है। इस तरह प्रत्येक नक्षत्र १३ डिग्री २० मिनट का होता है।
वैदिक ज्योतिष में राशियो को ३६० डिग्री को १२ भागो में बांटा गया है जिसे भचक्र कहते हैं। भचक्र में कुल 12 राशियां होती हैं। राशिचक्र में प्रत्येक राशि ३० डिग्री होती है। राशिचक्र में सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी इसलिए इसे पहला तारा माना जाता है। इसके बाद है भरणी फिर कृतिका इस प्रकार क्रमवार २७ नक्षत्र आते हैं। पहले दो नक्षत्र हैं अश्विनी और भरणी हैं जिनसे पहली राशि यानी मेष का निर्माण होता हैं इसी क्रम में शेष नक्षत्र भी राशियों का निर्माण करते हैं।
(ख) नवग्रह : वैदिक ज्योतिष में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरू, शुक्र, शनि और राहु केतु को नवग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त है। सभी ग्रह अपने गोचर मे भ्रमण करते हुए राशिचक्र में कुछ समय के लिए ठहरते हैं और अपना अपना राशिफल प्रदान करते हैं। राहु और केतु आभाषीय ग्रह है, नक्षत्र मंडल में इनका वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये दोनों राशिमंडल में गणीतीय बिन्दु के रूप में स्थित होते हैं।
(ग) लग्न और जन्म राशि : पृथ्वी अपने अक्ष पर २४ घंटे में एक बार पश्चिम से पूरब घूमती है। इस कारण से सभी ग्रह नक्षत्र व राशियां २४ घंटे में एक बार पूरब से पश्चिम दिशा में घूमती हुई प्रतीत होती है। इस प्रक्रिया में सभी राशियां और तारे २४ घंटे में एक बार पूर्वी क्षितिज पर उदित और पश्चिमी क्षितिज पर अस्त होते हुए नज़र आते हैं। यही कारण है कि एक निश्चित बिन्दु और काल में राशिचक्र में एक विशेष राशि पूर्वी क्षितिज पर उदित होती है। जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है उस समय उस अक्षांश और देशांतर में जो राशि पूर्व दिशा में उदित होती है वह राशि व्यक्ति का जन्म लग्न कहलाता है। जन्म के समय चन्द्रमा जिस राशि में बैठा होता है उस राशि को जन्म राशि या चन्द्र लग्न के नाम से जाना जाता है।
फलित ज्योतिष → (परंपरायें) (वर्तमान परंपराएँ) २. पश्चिमी ज्योतिष >>
२७ नक्षत्रों, १२ राशियों एवं ९ ग्रहों के सम्मिलन का गणितीय ढांचा तैयार होने पर भारतीय ज्योतिष गणन प्रारंभ होता है जिसका वास्तविक आधार चन्द्रमा को माना गया है कि जिस तरह से चन्द्रमा का हर पन्द्रह दिनों में बदलना होता है उसी के आधार पर ग्रहों के प्रभाव में भी बदलाव होता है एसा माना गया है, किन्तु इसके विपरीत पश्चिमी देशों में ९ के स्थान पैर १२ ग्रहों का सम्मिलन किया गया है तथा पश्चिमी देशों के गणितीय समीकरणों में सूर्या को आधार माना गया है।
फलित ज्योतिष → (परंपरायें) (वर्तमान परंपराएँ) ३. चीनी ज्योतिष >>
चीन में ज्योतिष का इतिहास पाँच हजार वर्ष से अधिक पुराना है। वहाँ के मनीषियों ने अपनी ज्योतिष विद्या को पौर्वात्य देशों में विस्तारित किया है। भारत ही नहीं, विश्व के अलग-अलग भू-भागों में मानव-सभ्यता और संस्कृति समानान्तर रूप से साथ-साथ जन्मीं और विकसित हुई हैं। मानव-विकास की गाथा अनबूझ रहस्यों की परतें खोलने कि दिशा में प्रेरित किया। रहस्य की परत-दर-परत खोलते हुए मानव अतल गहराईयों में उतरता चला गया। फलस्वरूप विकास और विज्ञान निरन्तर बढ़ता गया। तथाकथित ज्ञान बहुरूपों में प्रकट हुआ। विश्व के किसी भी भू-भाग में जन्मने और विकसित होनेवाला चाहे धर्म हो, योग हो, दर्शन-मनोविज्ञान हो, वेद-वेदांग या ज्योतिष या अन्य कोई विधा हो, उसका मूल्य उदेश्य आत्म-ज्ञान प्राप्त करना, उसकी दिशा में बढ़ना और बढ़ते जाना ही रहा है। अध्यात्म का लक्ष्य तो यही है। विधा कोई भी हो, ये सब आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु मानव द्वारा किये गए शताब्दियों नहीं, सहस्राब्दियों के ज्ञान-पिपासु प्रयासों के साक्षात् प्रमाण हैं। चीनी ज्योतिष के अन्तर्गत ‘पशु-नामांकित राशि-चक्र’ भी इसी मूल उद्देश्य की प्रतिपूर्ति करता है। चीन, जापान, कोरिया, वियतनाम आदि देशों में यह बहुप्रचलित है। भारत में इसका प्रचलन तो दूर, इसके बारे में भी बहुत कम लोग थोड़ा-बहुत जानते होंगे। तथा किसी भी भारतीय भाषा के लिए चीन का यह ज्ञान अपरिचित है।
चीनी ज्योतिष के अन्तर्गत ‘पशु-नामांकित राशि-चक्र’ में बारह राशियाँ हैं, जिन्हें चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम में ‘वर्ष’ या ‘सम्बन्धित पशु-वर्ष’ के नाम से पुकारते हैं। ऐसी धारणा है कि चीन में लगभग २००० साल पूर्व एक दिन, जिसे वियतनाम में ‘टेट’ कहा जाता है, चीन को संकट से उबारने के लिए भगवान बुद्ध ने सभी जानवरों को आमन्त्रित किया, किन्तु उस दिन वहाँ पर केवल बारह पशु ही पहुँचे-चूहा, बैल, चीता, बिल्ली, ड्रैगन, सर्प, अश्व, बकरी, वानर, मुर्ग, श्वान् यानी कुत्ता और सुअर। भगवान बुद्ध ने, जिस क्रम से ये पशु वहाँ पहुँचे थे, उसी क्रम में उन्हें वर्ष का अधिष्ठाता’ बना दिया; ये पशु-वर्ष हर बारह साल बाद पुनः चाक्रिकक्रम में वापस आ जाते हैं। भारतीय ज्योतिष की तरह इन एशियाई देशों की गणना चन्द्र-आधारित है। अन्तर यह है कि हमारे यहाँ एक राशि में ढाई दिन रहता है। जबकि चीन आदि देशों में यह गणना चान्द्र-वर्ष पर आधृत है- एक चान्द्र-वर्ष में १२ कृष्ण-पक्ष होते हैं १३वाँ बारह वर्ष बाद जुड़ता है- फलतः टेट का दिन कभी एक ही तारीख को नहीं पड़ता है।
फलित ज्योतिष → (परंपरायें) २ ऐतिहासिक परंपराएँ
अपने लंबे इतिहास के दौरान, ज्योतिष विज्ञान ने कई क्षेत्रों में शोहरत प्राप्त की और परिवर्तन के साथ-साथ इसमें विकास भी हुआ। ऐसी कई ज्योतिष परम्पराएं हैं जिनका ऐतिहासिक महत्त्व है, मगर आज वो बहुत कम प्रयोग में आते हैं। ज्योतिषियों की उनमें अभी भी रुचि बरकरार है और वे उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखते हैं। ज्योतिष के ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण परंपराओं में शामिल हैं:
- अरबी और फारसी ज्योतिष (मध्यकालीन मध्य पूर्व)
- बेबीलोन ज्योतिष(प्राचीन, मध्यपूर्व)
- मिस्र ज्योतिष
- हेलेनिस्टिक ज्योतिष (शास्त्रीय पुरातनता)
- मायां ज्योतिष
- पश्चिमी, चीनी और भारतीय ज्योतिष
फलित ज्योतिष → (परंपरायें) ३ गुप्त परंपराएं
अनेक सूफ़ी या गुप्त परंपराओं को ज्योतिष से जोड़ा गया है। कुछ मामलों में, जैसे कब्बाला में, ज्योतिष के अपने पारंपरिक तत्वों को प्रतिभागियों द्वारा इक्कठा करके अंतर्भूत किया जाता है। अन्य मामलों में, जैसे की आगम भविष्यवाणी में, बहुत से ज्योतिषी ज्योतिष के अपने काम में परम्पराओं को सम्मिलित करते हैं। गुप्त परंपराएं में निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं, लेकिन गुप्त परंपराएं इतने तक ही सीमित नहीं हैं:
- रसायन विद्या
- हस्तरेखा-शास्त्र
- गूढ़ ज्योतिष
- चिकित्सा ज्योतिष
- संख्या विज्ञान
- रोसिक्रुसियनया “रोज क्रॉस”
- टैरो द्वारा भविष्यकथन
इतिहास के अनुसार, पश्चिमी दुनिया में रसायन विद्या विशेषत: समवर्गी था और ज्योतिष की पारंपरिक बाबिल-यूनानी शैली से मिला हुआ था; कई मायनों में ये मनोगत या गुप्त ज्ञान को खोजने में एक दूसरे के पूरक थे। ज्योतिष ने रसायन विद्या की चार संस्थापित तत्वों की अवधारणा का प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान समय तक उपयोग किया है। परंपरागत रूप से, सौरमंडल के सात ग्रहों में से प्रत्येक का अपना प्रभुत्व क्षेत्र या अधिराज्य है और वो निश्चित धातु पर आधिपत्य रखता है।
फलित ज्योतिष → (राशि चक्र)
राशि चक्र, नक्षत्रों का एक घेरा या समूह है जिसके माध्यम से सूर्य, चंद्रमा और ग्रह आकाश में पारगमन करते हैं। ज्योतिषियों ने इन नक्षत्रों पर ध्यान दिया और उनको कुछ विशिष्ट महत्व दिया। समय के साथ-साथ उन्होंने बारहों नक्षत्रों की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर उस पर आधारित बारह राशि चिन्हों की एक प्रणाली बना ली।
- मेष (Aries)
- वृषभ (Taurus)
- मिथुन (Gemini)
- कर्क (Cancer)
- सिंह (Leo)
- कन्या (Virgo)
- तुला (Libra)
- वृश्चिक (Scorpio)
- धनु (Sagittarius)
- मकर (Capricorn)
- कुंभ (Aquarius)
- मीन (Pisces)
पश्चिमी और वैदिक राशि चक्रों का कुण्डलिनी ज्योतिष की परम्परा में एक ही मूल है, इसलिए दोनों एक दूसरे से बहुत से मायने में समान हैं। दूसरी ओर चीन में, राशि चक्र का अलग तरीके से विकास हुआ था। हालांकि चीनियों का भी एक बारह चिन्हों वाला तंत्र है (जानवरों के नाम पर आधारित), चीनी राशि चक्र शुद्ध पंचांग चक्र का हवाल देता है, इसमें पश्चिमी और भारतीय राशि चक्रों से जुड़ा हुआ कोई समकक्ष नक्षत्र नहीं है।
बारह राशि चक्रों की सर्वनिष्ठ बात ये है की सूर्य और चंद्रमा की अंतःक्रिया को ही ज्योतिष के सभी रूपों में केन्द्र माना गया है।
पश्चिमी ज्योतिषियों के एक बड़े हिस्से ने आकाश को ३० अंश के बारह बराबर खंडों में बाटने वाले उष्णकटिबंधीय राशि चक्र को अपने काम का आधार बनाया जिसकी शुरुआत मेष के पहले बिन्दु से होती है, जहाँ आकाशीय भूमध्य रेखा और क्रांतिवृत्त (आकाश के माध्यम से सूर्य के पथ), उत्तरी गोलार्द्ध के वलय विषुव पर मिलते हैं। विशुओं के पुरस्सरण के कारण, पृथ्वी का अंतरिक्ष में घूर्णन करने का रास्ता धीरे धीरे बदलता है, इस प्रणाली में राशि चक्र चिन्ह का समान नाम वाले नक्षत्र से कोई संबंध नहीं है, अपितु वो महीनों और ऋतुओं के संरेखन में (सीध में) रहते हैं।
वैदिक ज्योतिष की परम्परा का पालन करने वाले और अल्प संख्या में यानि कुछ पश्चिमी ज्योतिषी समान नक्षत्र राशि चक्र उपयोग करते हैं। यह राशि चक्र उसी समान रूप से विभाजित क्रांतिमण्डल का प्रयोग करता है लेकिन राशि चिन्हों के समान नाम वाले विचाराधीन नक्षत्रों की स्थिति के लगभग संरेखन में रहता है। नक्षत्र राशि चक्र उष्णकटिबंधीय राशि चक्र से अयानाम्सा कही जाने वाली दूरी से बराबर दूरी से अलग है, जो की विशुओं के झुकाव के साथ-साथ आगे बढ़ता है। इसके अलावा, कुछ नक्षत्र ज्ञाता (अर्थात् ज्योतिषी जो नक्षत्र तकनीक का प्रयोग करते हैं) वास्तविक, असमान राशिचक्रों के नक्षत्रों को अपने काम में इस्तेमाल करते हैं।
फलित ज्योतिष → (कुण्डलिनी ज्योतिष)
ज्योतिष घरों और ग्रहों एवं चिन्हों के लिए बनाऐ गये शिल्प के नमूने को प्रर्दशित करने वाली कुंडली ज्योतिष प्रणाली, भूमध्य क्षेत्र और विशेष रूप से हेलेनिस्टिक मिस्र के आस-पास के क्षेत्र में दूसरी या पहली शताब्दी के शुरूआती दौर में विकसित हुई। ये परम्परा समय के विशिष्ट क्षण पर स्वर्ग या कुंडली के द्वि- आयामी आरेख से सम्बद्ध है। यह चित्र विशेष नियमों और दिशा निर्देशों के आधार पर खगोलीय पिंडों के संरेखण में छिपे अर्थों को समझने के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं। एक कुंडली कि गणना सामान्यतः एक व्यक्ति विशेष के जन्म के समय या फिर किसी उद्यम या घटना के शुरुआत में कि जाती है, क्यूंकि उस समय के आकाशीय सरेखण को उन विषयों की प्रकृति का निर्धारक माना जाता है जिनके बारे में हम जानना चाहते हैं। ज्योतिष के इस रूप का एक विशिष्ट लक्षण जो इसे दूसरों से अलग करता है वो है परीक्षा के विशिष्ट क्षण, जिसे अन्यथा पधान के रूप में भी जाना जाता है। पर क्रांतिवृत्त की पृष्ठभूमि के सामने, पूर्वी क्षितिज की बढ़ने वाली डिग्री की गणना.कुंडली का ज्योतिष दुनिया भर में फैले ज्योतिष का सर्वाधिक प्रभावशाली रूप है, ख़ास तौर पर अफ्रीका, भारत, यूरोप और मध्य पूर्व में और भारतीय, मध्य कालीन और आधुनिक पश्चिम ज्योतिष सहित कुंडली ज्योतिष की कई मुख्य प्रथाएँ, हेलेनिस्टिक परम्पराओं से उत्त्पन्न हुई हैं
फलित ज्योतिष → (कुंडली)
कुण्डलिनी ज्योतिष का केन्द्र और उसकी शाखाएं, कुंडली या ज्योतिष के लेखाचित्र की गणना है। यह द्वि-आयामी रेखाचित्र प्रस्तुति, दिए गए समय और स्थान पर, पृथ्वी पर स्थिति के सहारे, स्वर्ग में आकाशीय पिंडों की आभासी स्थिति को दर्शाता है। कुंडली भी बारह विभिन्न खगोलीय गृहों में विभाजित हैं जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का निर्धारण करते हैं। कुंडली में जो गणना होती है उसमें गणित और सरल रेखागणित शामिल होती है जो की स्वर्गीय निकायों की स्पष्ट स्थिति और समय का खगोलीय सारणी पर आधारित होती है। प्राचीन हेलेनिस्टिक ज्योतिष में आरोह कुंडली के पहले आकाशीय गृह को परिलक्षित करता था। यूनानी में आरोह के लिए होरोस्कोपोस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था जिससे होरोस्कोप शब्द की उत्पत्ति हुई.आधुनिक समय में, यह शब्द ज्योतिष लेखा-चित्र को दर्शाता है।
फलित ज्योतिष → (कुंडली ज्योतिष की शाखाएं)
कुंडली ज्योतिष की परम्पराओं को चार शाखाओं में विभाजित किया जा सकता है जो की विशिष्ट विषयों या उद्देश्यों की ओर निर्दिष्ट हैं। अक्सर, ये शाखाएं एक अनूठे प्रकार की तकनीकों का समुच्चय या फिर भिन्न क्षेत्र के लिए प्रणाली के मूल सिद्धांतों के विभिन्न प्रयोगों का इस्तेमाल करती हैं। ज्योतिष के कई अन्य उप-समुच्चयों और प्रयोगों का आरम्भ चार मौलिक शाखाओं से हुआ है।
फलित ज्योतिष → (नवजात ज्योतिष)
व्यक्ति की जन्म-पत्री का अध्ययन है जिसके आधार पर व्यक्ति के बारे में और उसके जीवन के अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है।
फलित ज्योतिष → (कतार्चिक ज्योतिष)
कतार्चिक ज्योतिष में चुनावी और घटना ज्योतिष दोनों शामिल हैं। इनमें से पहले ज्योतिष में ज्योतिष के ज्ञान का उपयोग किसी उद्यम या उपक्रम को शुरू करने के लिए शुभ घड़ी का पता लगाने के लिए किया जाता है और बाद वाले का उपयोग किसी घटना के होने के समय से उस घटना के बारे में सब कुछ समझने के लिए किया जाता है।
फलित ज्योतिष → (प्रतिघंटा ज्योतिष)
प्रतिघंटा ज्योतिष में ज्योतिषी किसी प्रश्न का जवाब, उस प्रश्न को पूछे जाने के क्षण का अध्धयन करके देता है।
फलित ज्योतिष → (सांसारिक या विश्व ज्योतिष)
मौसम, भूकंप और धर्म या राज्यों के उन्नयन एवं पतन सहित दुनिया में होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए ज्योतिष का अनुप्रयोग. इसमें ज्योतिष युग, जैसे की कुंभ युग, मीन युग, इत्यादि शामिल हैं। प्रत्येक युग की लम्बाई लगभग २,१५० साल होती है और दुनिया में कई लोग इन महायुगों को ऐतिहासिक और वर्तमान घटनाओं से सम्बद्ध मानते हैं।
(४). अंक ज्योतिष
अनेक प्रणालियों, परम्पराओं, विश्वासों में अंक विद्या, अंकों और भौतिक वस्तुओं, जीवित वस्तुओं के बीच एक रहस्यवाद, गूढ सम्बन्ध है।
आज, अंक विद्या को बहुत बार अदृश्य के साथ-साथ ज्योतिष विद्या और इसके जैसे शकुन विचारों की कलाओं से जोड़ा जाता है। इस शब्द को उनके लोगों के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है जो कुछ प्रेक्षकों के विचार में, अंक पद्धति पर ज्यादा विश्वास करते हैं, तब भी यदि वे लोग परम्परागत अंक विद्या को व्यव्हार में नहीं लाते। उदाहरण के लिए, उनकी १९९७ की पुस्तक अंक विद्या, पाइथागोरस ने क्या गढ़ा, गणितज्ञ अंडरवुड डुडले ने शेयर बाजार विश्लेषण के एलिअट के तरंग सिद्धांत के प्रयोगकर्ताओं की चर्चा करने के लिए इस शब्द का उपयोग किया है।
आधुनिक अंक विद्या में कई बार प्राचीन संस्कृति और शिक्षकों की विविधताओं के पहलुओं का उल्लेख है जिसमें बेबीलोनया, पाइथागोरस और उनके अनुयायी (ग्रीस, 6 वीं शताब्दी ई.पू.), हेलेनिस्टिक एलेक्सेन्ड्रिया, प्रारंभिक ईसाई रहस्यवाद, प्रारंभिक गूढ़ ज्ञानवाद का रहस्य, कबालाह की यहूदी परम्परा, भारतीय वेद, चीन का मृत लोगों का घेरा और इजिप्ट की रहस्यमय घर के मालिक की पुस्तक (मृतक के संस्कार) शामिल हैं।
पाइथागोरस और उस समय के अन्य दार्शनिकों का यह मानना था कि भौतिक अवधारणाओं की तुलना में गणितीय अवधारणाओं में अधिक व्यवहारिकता (नियमित और वर्गीकरण में आसान) थी, इसलिए उनमें अधिक वास्तविकता थी।
हिप्पो के संत आगस्टिन (ऐ डी ३५४-४३०) ने लिखा है, “अंक सार्वलौकिक भाषा हैं, जो परमात्मा द्वारा सत्य की पुष्टि में हमें प्रदान किए गए हैं।” पाइथागोरस की ही तरह, वे भी यह मानते थे कि प्रत्येक वस्तु में संख्यात्मक सम्बन्ध है और यह मस्तिष्क पर था कि वह इन संबंधों के रहस्यों की जाँच कर इनका पता लगाये या फिर ईश्वर की अनुकंपा से यह रहस्य खुलने दे।
३२५ एडी में, नीकैया की पहली परिषद् के बाद, रोमन साम्राज्य में नागरिक उपद्रव होने के कारण राज्य चर्च पर से विश्वास उठने लगा था। अंक विद्या को ईसाई प्राधिकारी से मान्यता नहीं मिली और इसे शकुन के अन्य रूपों और जादू टोनों के साथ अमान्य विश्वासों के क्षेत्र में रख दिया गया। इस धार्मिक शुद्धिकरण के द्वारा, अब तक “पवित्र” संख्याओं को जो महत्व दिया जाता था, वह ख़त्म होने लगा। फिर भी, अनेक संख्याओं, जैसे यीशु संख्या पर टिप्पणी की गई है और यह गाजा के डोरोथ्स द्वारा विश्लेषित की गयी है और रुढीवादी ग्रीक क्षेत्रों में अब भी अंक विद्या का प्रयोग किया जाता है
अंग्रेजी साहित्य में अंक विद्या के प्रभाव का एक उदाहरण है, १६५८ में सर थॉमस ब्राउन का डिस्कोर्स दी गार्डन ऑफ़ सायरस इसमें लेखक ने कला, प्रकृति और रहस्यवाद में हर तरफ़ पाँच अंक और सम्बंधित क्विन्क्न्क्स शैली का वर्णन किया है।
आधुनिक अंक विद्या में अनेक पूर्व वृत्तान्त है। रुथ एड्रायर की पुस्तक, अंक विद्या, अंकों की शक्ति (स्क्वायर वन प्रकाशक) का कहना है कि इस सदी के बदलने तक (१८०० से १९०० ई. के लिए) श्रीमती एल डॉव बेलिएट ने पाइथागोरस ‘ के कार्य को बाइबिल के संदर्भ के साथ सयुंक्त कर दिया था। फिर १९७० के मध्य तक, बेलिएट के एक विद्यार्थी, डॉ॰ जूनो जॉर्डन ने उस अंक विद्या को और परिवर्तित किया और वह प्रणाली विकसित करने में सहयोग दिया जो आज “प्य्थागोरियन” के नाम से जानी जाती है।
अंक ज्योतिष → (अंक परिभाषाएँ)
विशेष अंकों के अर्थों के लिए कोई परिभाषाएँ निर्धारित नहीं है। सामान्य उदाहरणों में शामिल हैं :
- ०. सब कुछ या सम्पूर्णता सब
- १. व्यक्तिगत हमलावर यांग
- २. संतुलन. यूनियन. ग्रहणशील यिन
- ३. संचार/अन्योन्यक्रियातटस्थता
- ४. सृजन
- ५. कार्य बेचैनी
- ६. प्रतिक्रिया/ प्रवाहदायित्व
- ७. विचार/चेतना
- ८. अधिकार/त्याग
- ९. पूर्णता
- १० .पुनर्जन्म
अंक ज्योतिष → (अंकों को जोड़ना)
अंक वैज्ञानिक बहुत बार एक संख्या या शब्द को एक प्रक्रिया द्वारा कम कर देते हैं, जिसे अंकों को जोड़ना कहा जाता है, फिर प्राप्त एकल अंक के आधार पर निष्कर्ष तक पहुँचते हैं।
अंकों को जोड़ने में, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एक संख्या के सभी अंकों का योग किया जाता है और जब तक एकल अंक का जवाब नहीं मिल जाता तब तक इस प्रक्रिया को दोहराया जाता है। एक शब्द के लिए, वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर के स्थान से सम्बद्ध मान को लिया जाता है (जैसे, एक =१, बी=२, से लेकर जेड़ = २६) को जोर जाता है।
उदाहरण : ३.४८९ → ३ + ४ + ८ + ९ = २४ → २ + ४ = ६
→ ८ + ५ + १२ + १२ + १५ = ५२ → ५ + २ = ७
एक एकल अंक के योग पर पहुँचने का सबसे तेज तरीका है, ९ से ० परिणाम को बदलकर सिर्फ़ मान माडुलो ९, प्राप्त करना।
गणना की विभिन्न विधियां उपलब्ध है, जिनमे शाल्डियन, पैथोगोरियन, हेब्रैक हेलीन हिचकॉक की विधि, ध्वन्यात्मक, जापानी और भारतीय शामिल है। रुथ एब्राम्स ड्रायर की पुस्तक के अनुसार, अंक विद्या, अंकों की शक्ति, यदि आप एक ऐसे देश में जन्मे हो जहाँ की मात्र भाषा अंग्रेजी नहीं थी, तो आप अपनी स्वयं की शब्दमाला लें और उसे उन्ही निर्देशों के अनुसार अक्षर क्रम में जमा लें जिस प्रकार अंग्रेजी शब्दमाला के अनुसार बताया गया है।
ऊपर दिए गए उदाहरणों में दशमलव (आधार १०) अंकगणित का प्रयोग कर गणना की गयी है। अन्य संख्या प्रणाली भी हैं, जैसे द्विआधारी, अष्टाधारी, षोडश आधारी और वीगेसीमल, इनके आधार पर संख्याओं को जोड़ने पर अलग-अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। ऊपर दर्शित पहला उदाहरण, इस प्रकार दिखेगा जब अष्टाधारी (आधार ८) के अनुसार गणना की गई है :
३.४८९१० = ६६४१८ → ६ + ६ + ४ + १ = २१८ → २ + १ = ३८ = ३१०
अंक ज्योतिष → (अंग्रेजी अक्षर संख्यात्मक मूल्य)
अंक ज्योतिष → (अंग्रेजी अक्षरों के संख्यात्मक मान विधि ; शाल्डियन विधि)
० से ९ तक का प्रत्येक अंक हमारे सौर मंडल की एक दिव्य शक्ति द्वारा नियंत्रित है।
अनेक रसविद्या सिद्धांतों का अंक विद्या से निकट का सम्बन्ध था। आज भी इस्तेमाल में आने वाली अनेक रासायनिक प्रक्रियाओं के आविष्कारक, फारस रस्वैध्य जाबिर इब्न हैयान, ने अपने प्रयोग अरबी भाषा में पदार्थों के नामों पर आधारित अंक विद्या पर आधारित किए।
विज्ञान के क्षेत्र में “अंक विद्या” के सबसे अधिक ज्ञात उदाहरण में शामिल है, कुछ निश्चित बड़ी संख्याओं की समानता का संयोग, जिसने गणितीय भौतिक वैज्ञानिकों पॉल डिराक, गणितज्ञ हर्मन वेल और खगोलज्ञ आर्थर स्टैनले एडिंग्टन जैसे प्रतिष्ठित लोगों को अपने जाल में ले लिया। ये संख्यात्मक संयोग ऐसी मात्राओं का जिक्र करते हैं जैसे ब्रह्मांड की आयु और समय की परमाणु इकाई का अनुपात, ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए गुरुत्व बल और विद्युत बल की शक्ति में अन्तर।
(५). खगोलशास्त्र
खगोल शास्त्र, एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी और उसके वायुमण्डल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण तथा उसकी व्याख्या की जाती है। यह वह अनुशासन है जो आकाश में अवलोकित की जा सकने वाली तथा उनका समावेश करने वाली क्रियाओं के आरंभ, बदलाव और भौतिक तथा रासायनिक गुणों का अध्ययन करता है।
खगोलिकी ब्रह्मांड में अवस्थित आकाशीय पिंडों का प्रकाश, उद्भव, संरचना और उनके व्यवहार का अध्ययन खगोलिकी का विषय है। अब तक ब्रह्मांड के जितने भाग का पता चला है उसमें लगभग १९ अरब आकाश गंगाओं के होने का अनुमान है और प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग १० अरब तारे हैं। आकाश गंगा का व्यास लगभग एक लाख प्रकाशवर्ष है। हमारी पृथ्वी पर आदिम जीव २ अरब साल पहले पैदा हुआ और आदमी का धरती पर अवतण १०-२० लाख साल पहले हुआ।
वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महापिंड के विस्फोट से हुई है। सूर्य एक औसत तारा है जिसके आठ मुख्य ग्रह हैं, उनमें से पृथ्वी भी एक है। इस ब्रह्मांड में हर एक तारा सूर्य सदृश है। बहुत-से तारे तो ऐसे हैं जिनके सामने अपना सूर्य अणु (कण) के बराबर भी नहीं ठहरता है। जैसे सूर्य के ग्रह हैं और उन सबको मिलाकर हम सौर परिवार के नाम से पुकारते हैं, उसी प्रकार हरेक तारे का अपना अपना परिवार है। बहुत से लोग समझते हैं कि सूर्य स्थिर है, लेकिन संपूर्ण सौर परिवार भी स्थानीय नक्षत्र प्रणाली के अंतर्गत प्रति सेकेंड १३ मील की गति से घूम रहा है। स्थानीय नक्षत्र प्रणाली आकाश गंगा के अंतर्गत प्रति सेकेंड २०० मील की गति से चल रही है और संपूर्ण आकाश गंगा दूरस्थ बाह्य ज्योर्तिमालाओं के अंतर्गत प्रति सेकेंड १०० मील की गति से विभिन्न दिशाओं में घूम रही है।
चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है जिस पर मानव के कदम पहुँच चुके हैं। इस ब्रह्मांड में सबसे विस्मयकारी दृश्य है, आकाश गंगा (गैलेक्सी) का दृश्य। रात्रि के खुले (जब चंद्रमा न दिखाई दे) आकाश में प्रत्येक मनुष्य इन्हें नंगी आँखों से देख सकता है। देखने में यह हल्के सफेद धुएँ जैसी दिखाई देती है, जिसमें असंख्य तारों का बाहुल्य है। यह आकाश गंगा टेढ़ी-मेढ़ी होकर बही है। इसका प्रवाह उत्तर से दक्षिण की ओर है। पर प्रात:काल होने से थोड़ा पहले इसका प्रवाह पूर्वोत्तर से पश्चिम और दक्षिण की ओर होता है। देखने में आकाश गंगा के तारे परस्पर संबद्ध से लगते हैं, पर यह दृष्टि भ्रम है। एक दूसरे से सटे हुए तारों के बीच की दूरी अरबों मील हो सकती है। जब सटे हुए तारों का यह हाल है तो दूर दूर स्थित तारों के बीच की दूरी ऐसी गणनातीत है जिसे कह पाना मुश्किल है। इसी कारण से ताराओं के बीच तथा अन्य लंबी दूरियाँ प्रकाशवर्ष में मापी जाती हैं। एक प्रकाशवर्ष वह दूरी है जो दूरी प्रकाश एक लाख छियासी हजार मील प्रति सेकेंड की गति से एक वर्ष में तय करता है। उदाहरण के लिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सवा नौ करोड़ मील है, प्रकाश यह दूरी सवा आठ मिनट में तय करता है। अत: पृथ्वी से सूर्य की दूरी सवा आठ प्रकाश मिनट हुई। जिन तारों से प्रकाश आठ हजार वर्षों में आता है, उनकी दूरी हमने पौने सैंतालिस पद्म मील आँकी है। लेकिन तारे तो इतनी इतनी दूरी पर हैं कि उनसे प्रकाश के आने में लाखों, करोड़ों, अरबों वर्ष लग जाता है। इस स्थिति में हमें इन दूरियों को मीलों में व्यक्त करना संभव नहीं होगा और न कुछ समझ में ही आएगा। इसीलिए प्रकाशवर्ष की इकाई का वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया है।
मान लीजिए, ब्रह्मांड के किसी और नक्षत्रों आदि के बाद बहुत दूर दूर तक कुछ नहीं है, लेकिन यह बात अंतिम नहीं हो सकती है। यदि उसके बाद कुछ है तो तुरंत यह प्रश्न सामने आ जाता है कि वह कुछ कहाँ तक है और उसके बाद क्या है? इसीलिए हमने इस ब्रह्मांड को अनादि और अनंत माना। इसके अतिरिक्त अन्य शब्दों में ब्रह्मांड की विशालता, व्यापकता व्यक्त करना संभव नहीं है।
अंतरिक्ष में कुछ स्थानों पर दूरदर्शी से गोल गुच्छे दिखाई देते हैं। इन्हें स्टार क्लस्टर या ग्लीट्य्रूलर स्टार अर्थात् तारा गुच्छ कहते हैं। इसमें बहुत से तारे होते हैं जो बीच में घने रहते हैं और किनारे बिरल होते हैं। टेलिस्कोप से आकाश में देखने पर कहीं कहीं कुछ धब्बे दिखाई देते हैं। ये बादल के समान बड़े सफेद धब्बे से दिखाई देते हैं। इन धब्बों को ही नीहारिका कहते हैं। इस ब्रह्मांड में असंख्य नीहारिकाएँ हैं। उनमें से कुछ ही हम देख पाते हैं।
इस अपरिमित ब्रह्मांड का अति क्षुद्र अंश हम देख पाते हैं। आधुनिक खोजों के कारण जैसे जैसे दूरबीन की क्षमता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ब्रह्मांड के इस दृश्यमान क्षेत्र की सीमा बढ़ती जाती है। परन्तु वर्तमान परिदृश्य में ब्रह्मांड की पूरी थाह मानव क्षमता से बहुत दूर है।
खगोल भौतिकी का आधुनिक युग जर्मन भौतिकविद् किरचाक से आरंभ हुआ। सूर्य के वातावरण में सोडियम, लौह, मैग्नेशियम, कैल्शियम तथा अनेक अन्य तत्वों का उन्होंने पता लगाया (सन् १८५९)। हमारे देश में स्वर्गीय प्रोफेसर मेघनाद साहा ने सूर्य और तारों के भौतिक तत्वों के अध्ययन में महत्वपूर्ण कार्य किया है। उन्होंने वर्णक्रमों के अध्ययन से खगोलीय पिंडों के वातावरण में अत्यंत महत्वपूर्ण खोजें की हैं। आजकल भारत गणराज्य के दो प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ॰ एस. चंद्रशेखर और डॉ॰ जयंत विष्णु नारलीकर भी ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में उलझे हुए हैं।
बहुत पहले कोपर्निकस, टाइको ब्राहे और मुख्यत: कैप्लर ने खगोल विद्या में महत्वपर्णू कार्य किया था। कैप्लर ने ग्रहों के गति के संबंध में जिन तीन नियमों का प्रतिपादन किया है वे ही खगोल भौतिकी की आधारशिला बने हुए हैं। खगोल विद्या में न्यूटन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण रहा है।
ब्रह्मांड विद्या के क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों (लगभग ४५ वर्षों पूर्व) की खोजों के फलस्वरूप कुछ महत्वपूर्ण बातें समाने आई हैं। विख्यात वैज्ञानिक हबल ने अपने निरीक्षणों से ब्रह्मांडविद्या की एक नई प्रक्रिया का पता लगाया। हबल ने सुदूर स्थित आकाश गंगाओं से आनेवाले प्रकाश का परीक्षण किया और बताया कि पृथ्वी तक आने में प्रकाश तरंगों का कंपन बढ़ जाता है। यदि इस प्रकाश का वर्णपट प्राप्त करें तो वर्णपट का झुकाव लाल रंग की ओर अधिक होता है। इस प्रक्रिया को डोपलर प्रभाव कहते हैं। ध्वनि संबंधी डोपलर प्रभाव से बहुत लोग परिचित होंगे। जब हम प्रकाश के संदर्भ में डोपलर प्रभाव को देखते हैं तो दूर से आनेवाले प्रकाश का झुकाव नीले रंग की ओर होता है और दूर जाने वाले प्रकाश स्रोत के प्रकाश का झुकाव लाल रंग की ओर होता है। इस प्रकार हबल के निरीक्षणों से यह मालूम हुआ कि आकाश गंगाएँ हमसे दूर जा रही हैं। हबल ने यह भी बताया कि उनकी पृथ्वी से दूर हटने की गति, पृथ्वी से उनकी दूरी के अनुपात में है। माउंट पोलोमर वेधशाला में स्थित २०० इंच व्यासवाले लेंस की दूरबीन से खगोल शास्त्रियों ने आकाश गंगाओं के दूर हटने की प्रक्रिया को देखा है।
दूरबीन से ब्रह्मांड को देखने पर हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हम इस ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु हैं और बाकी चीजें हमसे दूर भागती जा रही हैं। यदि अन्य आकाश गंगाओं में प्रेक्षक भेजे जाएँ तो वे भी यही पाएंगे कि इस ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु हैं, बाकी आकाश गंगाएँ हमसे दूर भागती जा रही हैं। अब जो सही चित्र हमारे सामने आता है, वह यह है कि ब्रह्मांड का समान गति से विस्तार हो रहा है। और इस विशाल प्रारूप का कोई भी बिंदु अन्य वस्तुओं से दूर हटता जा रहा है।
हबल के अनुसंधान के बाद ब्रह्मांड के सिद्धांतों का प्रतिपादन आवश्यक हो गया था। यह वह समय था जब कि आइन्सटीन का सापेक्षवाद का सिद्धांत अपनी शैशवावस्था में था। लेकिन फिर भी आइन्सटीन के सिद्धांत को सौरमंडल संबंधी निरीक्षणों पर आधारित निष्कर्षों की व्याख्या करने में न्यूटन के सिद्धांतों से अधिक सफलता प्राप्त हुई थी। न्यूटन के अनुसार दो पिंडों के बीच की गुरु त्वाकर्षण शक्ति एक दूसरे पर तत्काल प्रभाव डालती है लेकिन आइन्सटीन ने यह साबित कर दिया कि पारस्परिक गुरु त्वाकर्षण की शक्ति की गति प्रकाश की गति के समान तीव्र नहीं हो सकती है। आखिर यहाँ पर आइन्सटीन ने न्यूटन के पत्र को गलत प्रमाणित किया। लोगों को आइन्सटीन का ही सिद्धांत पसंद आया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की तीन धारणाएँ प्रस्तुत हैं –
- १. स्थिर अवस्था का सिद्धांत
- २. विस्फोट सिद्धांत (बिग बंग सिद्धांत) और
- ३. दोलन सिद्धांत।
इन धारणाओं में दूसरी धारणा की महत्ता अधिक है। इस धारणा के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक महापिंड के विस्फोट से हुई है और इसी कारण आकाश गंगाएँ हमसे दूर भागती जा रही है। इस ब्रह्मांड का उलटा चित्र आप अपने सामने रखिए तब आपको ब्रह्मांड प्रसारित न दिखाई देकर सकुंचित होता हुआ दिखाई देगा और आकाश गंगाएँ भागती हुई न दिखाई देकर आती हुई प्रतीत होगी। अत: कहने का तात्पर्य यह है कि किसी समय कोई महापिंड रहा होगा और उसी के विस्फोट होने के कारण आकाश गंगाएँ भागती हुई हमसे दूर जा रही हैं। क्वासर और पल्सर नामक नए तारों की खोज से भी विस्फोट सिद्धांत की पुष्टि हो रही है।
सभी प्राकृतिक विज्ञानों में से खगोलिकी सबसे प्राचीन है। इसका आरम्भ प्रागैतिहासिक काल से हो चुका था तथा प्राचीन धार्मिक एवं मिथकीय कार्यों में इसके दर्शन होते हैं। खगोलिकी के साथ फलित ज्योतिष का बहुत ही नजदीकी सम्बन्ध रहा है और आज भी जनता दोनो को अलग नहीं कर पाती। खगोलिकी (सिद्धान्त ज्योतिष) और फलित ज्योतिष केवल कुछ शताब्दी पहले ही एक-दूसरे से अलग हुए हैं।
प्राचीन खगोलविद तारों और ग्रहों के बीच के अन्तर को समझते थे। तारे शताब्दियों तक लगभग एक ही स्थान पर बने रहते हैं जबकि ग्रह कम समय में भी अपने स्थान से हटे हुए दिख जाते हैं।
खगोलशास्त्र → (खगोलीय यांत्रिकी)
खगोलीय यांत्रिकी में आकाशीय पिंडों की गतियों के गणितीय सिद्धांतों का विवेचन किया जाता है। न्यूटन द्वारा प्रिंसिपिया में उपस्थापित गुरुत्वाकर्षण नियम तथा तीन गतिनियम खगोलीय यांत्रिकी के मूल आधार हैं। इस प्रकार इसमें विचारणीय समस्या द्वितीय वर्ण के सामान्य अवकल समीकरणों के एक वर्ग के हल करने तक सीमित हो जाती है।
खगोलशास्त्र → (खगोलीय स्पेक्ट्रमिकी)
खगोलीय स्पेक्ट्रमिकी वह विज्ञान है जिसका उपयोग आकाशीय पिंडों के परिमंडल की भौतिक अवस्थाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। प्लैस्केट के मतानुसार भौतिकविद् के लिए स्पेक्ट्रमिकी वृहद् शस्त्रागार में रखे हुए अनेक अस्त्रों में से एक अस्त्र है। खगोल भौतिकविद् के लिए आकाशीय पिंडों के परिमंडल की भौतिक अवस्थाओं के अध्ययन का यह एकमात्र साधन है।
खगोलशास्त्र → (खगोलभौतिकी)
खगोलभौतिकी खगोल विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत खगोलीय पिंडो की रचना तथा उनके भौतिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। कभी-कभी इसे ‘ताराभौतिकी’ भी कह दिया जाता है हालाँकि वह खगोलभौतिकी की एक प्रमुख शाखा है जिसमें तारों का अध्ययन किया जाता है।
खगोलशास्त्र → (ताराभौतिकी)
ताराभौतिकी खगोलभौतिकी की एक शाखा है जो तारों से सम्बन्धित भौतिकी का अध्ययन करती है। इसमें तारों के जन्म, उनके क्रम-विकास के अन्तर्गत जीवन-चक्र, उनके ढांचे और अन्य पहलुओं पर जानकारी प्राप्त की जाती है।
खगोलशास्त्र → (खगोलशास्त्र से सम्बन्धित शब्दावली)
खगोलशास्त्र वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसका सबंध पृथ्वी के वातावरण के बाहर उत्पन्न होने वाले खगोलीय पिंडों और घटनाओं से होता है।
- अयन गति (Axial precession (astronomy))
- अंगिरस तारा (Epsilon Ursae Majoris)
- अंडाकार आकाशगंगा (Elliptical galaxy)
- अभिजित् तारा (Vega)
- अंतरतारकीय बादल (Interstellar cloud)
- अंतरतारकीय माध्यम (Interstellar medium)
- अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी वर्ष (International Year of Astronomy)
- अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (International Astronomical Union)
- अंतरिक्ष यान (Spacecraft)
- अम्ब्रिअल (उपग्रह) (Umbriel (moon))
- अधोरक्त खगोलशास्त्र (Infrared astronomy)
- अरुण के उपग्रह (Moons of Uranus)
- अरुण (Uranus)
- अब्द अल-रहमान अल-सूफ़ी (Abd al-Rahman al-Sufi)
- आकाश (Sky)
- आकाशगंगा (Galaxy)
- आकाशगंगीय सेहरा (Galactic halo)
- आद्रा तारा (Betelgeuse)
- आदिग्रह चक्र (Protoplanetary disk)
- आदि भीषण बमबारी (Late Heavy Bombardment)
- आन्ध्र पदार्थ (Dark matter)
- आणविक बादल (Molecular cloud)
- आयो (उपग्रह) (Io (moon))
- उदयपुर सौर वेधशाला (Udaipur Solar Observatory (USO))
- उपग्रह (Satellites)
- उपग्रही छल्ला (Planetary ring)
- उल्का (Meteoroid)
- एक्सोमार्स (ExoMars)
- एरेसिबो वेधशाला (Arecibo Observatory)
- एंड्रोमेडा आकाशगंगा (Andromeda Galaxy)
- ऐमलथीया (उपग्रह) (Amalthea (moon))
- ऍरिअल (उपग्रह) (Ariel (moon))
- ऍरिस (बौना ग्रह) (Eris (dwarf planet))
- ऐल्बीडो (Albedo)
- एन. जी. सी. (NGC)
- ऍस/२०११ पी १ (उपग्रह) (S/2011 P 1)
- ओबेरॉन (उपग्रह) (Oberon (moon))
- ओलम्पस मोन्स (Olympus Mons)
- और्ट बादल (Oort Cloud)
- कक्षा (Orbit)
- कक्षीय विकेन्द्रता (Orbital eccentricity)
- कॅप्लर-१६ तारा (Kepler-16)
- कॅप्लर-१६ बी (Kepler-16b)
- कॅप्लर-२२ तारा (Kepler-22)
- कॅप्लर-२२ बी (Kepler-22b)
- कॅप्लर अंतरिक्ष यान (Kepler (spacecraft))
- काइपर घेरा (Kuiper belt)
- काला बौना (Black dwarf)
- किन्नर (हीन ग्रह) (Centaur (minor planet))
- कॉरोना (Corona)
- कृत्तिका (Pleiades)
- क्वासर (Quasar)
- केप्लर के ग्रहीय गति के नियम (Kepler’s laws of planetary motion)
- कलिस्टो (उपग्रह) (Callisto (moon))
- क्षुद्रग्रह घेरा (Asteroid belt)
- क्षुद्रग्रह (Asteroid)
- खगोलभौतिकी (Astrophysics)
- खगोलशास्त्र (Astronomy)
- खगोलशास्त्री (Astronomers)
- खगोलीय इकाई (Astronomical unit)
- खगोलीय चिन्ह (Astronomical symbols)
- खगोलीय धूल (Cosmic dust)
- खगोलीय मैग्निट्यूड (Magnitude (astronomy))
- खगोलीय वस्तु (Celestial body)
- खगोलीय यांत्रिकी (Celestial mechanics)
- खगोलीय स्पेक्ट्रमिकी (Astronomical spectroscopy)
- खुला तारागुच्छ (Open cluster)
- गांगेय वर्ष (Galactic year)
- गोल तारागुच्छ (Globular cluster)
- गुप्त ऊर्जा (Dark energy)
- गुरुत्वाकर्षक लेंस (Gravitational lens)
- ग़ैर-सौरीय ग्रह (Extrasolar planet)
- गैलीलियो गैलिली (Galileo Galilei)
- गैनिमीड (उपग्रह) (Ganymede (moon))
- गैस दानव (Gas giant)
- ग्रह (Planet)
- ग्रहण (Eclipse)
- ग्रहीय मण्डल (planetary system)
- ग्रहीय वासयोग्यता (Planetary habitability)
- चंद्रा एक्स-रे वेधशाला (Chandra X-ray Observatory)
- चन्द्रमा (Moon)
- चंद्रग्रहण (Lunar eclipse)
- छोटा मॅजलॅनिक बादल (Small Magellanic Cloud)
- ज्वारभाटा बल (Tidal force)
- जेम्स वेब खगोलीय दूरदर्शी (James Webb Space Telescope (JWST))
- जुपिटर (Jupiter (mythology))
- जूनो (अंतरिक्ष यान) (Juno (spacecraft))
- ज्येष्ठा तारा (Antares)
- क्रांति (Declination)
- डन्डीय सर्पिल आकाशगंगा (Barred spiral galaxy)
- डिमोज़ (उपग्रह) (Deimos (moon))
- डेल्टा-v (Delta-v)
- ध्रुव तारा (Polaris, North star)
- ध्रुवमत्स्य (Little Bear or Ursa Minor)
- टाइटन (चंद्रमा) (Titan (moon))
- टाइटेनिआ (उपग्रह) (Titania (moon))
- टाईटन तृतीय ई (Titan IIIE)
- तारा गुच्छ (Star Cluster)
- तारा (Star)
- ताराघर (Planetarium)
- तारामंडल (Constellation)
- तारापुंज (Asterism (astronomy))
- तारों की श्रेणियाँ (Stellar classification)
- दक्षिण मीन तारामंडल (Piscis Austrinus)
- दिगंश (Azimuth)
- दिक् (Space)
- दिक्-काल (Space-Time)
- द्वितारा (Binary star)
- दोहरा तारा (Double star)
- दूरदर्शी (Telescope)
- दैनिक गति (Diurnal motion)
- धनु तारामंडल (Sagittarius (constellation))
- धूमकेतु (Comet)
- ध्रुव तारा (Pole star)
- ध्रुवमत्स्य तारामंडल (Ursa Minor)
- ध्रुवीय कक्षा (Polar orbit)
- ध्रुवीय ज्योति (Aurora)
- नक्षत्र (Nakshatra)
- नासा (NASA)
- निकोलस कोपरनिकस (Nicolaus Copernicus)
- नीहारिका (Nebula)
- निरपेक्ष कांतिमान (Absolute magnitude)
- निक्स (उपग्रह) (Nix (moon))
- न्यू होराएज़न्ज़ (New Horizons)
- पक (उपग्रह) (Puck (moon))
- परिध्रुवी तारा (Circumpolar star)
- पर्णिन अश्व तारामंडल (Pegasus (constellation))
- पारसैक (Parsec)
- पायोनियर कार्यक्रम (Pioneer program)
- पायोनियर १० (Pioneer 10)
- पायोनियर ११ (Pioneer 11)
- पृथ्वी (Earth)
- पृथ्वी द्रव्यमान (Earth mass)
- प्रकाश का विपथन (Aberration of light)
- प्रकाश-वर्ष (Light-year)
- प्रहार क्रेटर (Impact crater)
- प्रतिगामी चाल (Apparent retrograde motion)
- प्राकृतिक उपग्रह (Natural satellite)
- फ़ोबस (उपग्रह) (Phobos (moon))
- फ़ुमलहौत बी (Fomalhaut b)
- बायर नामांकन (Bayer designation)
- बेढंगी आकाशगंगा (Irregular galaxy)
- बिखरा चक्र (Scattered
- बिग बैंग सिद्धांत (Big Bang Theory)
- बृहस्पति (Jupiter)
- बृहस्पति का वायुमंडल (Atmosphere of Jupiter)
- बृहस्पति के प्राकृतिक उपग्रह (Moons of Jupiter)
- बौना ग्रह (Dwarf planet)
- बौनी आकाशगंगा (Dwarf galaxy)
- ब्रह्माण्ड-उत्पत्ति (Cosmogony)
- ब्रह्माण्ड किरण (Cosmic ray)
- ब्रह्माण्ड पुराण (Brahmanda Purana)
- ब्रह्माण्ड (Universe)
- ब्रह्माण्डविद्या (Cosmology)
- ब्लैक होल (काला छिद्र), (Black hole)
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)
- भूम्युच्च (Apogee)
- भूरा बौना (Brown dwarf)
- महाकुंचन (Big Crunch)
- महापृथ्वी (Super-Earth)
- माकेमाके (बौना ग्रह) (Makemake (dwarf planet))
- मार्स एक्सप्रेस (Mars Express)
- मार्स ओडिसी (Mars Odyssey)
- मेरिनर ४ (Mariner 4)
- मेरिनर ९ (Mariner 9)
- मॅजलॅनिक बादल (Magellanic Clouds)
- मंगल के उपग्रह (Moons of Mars)
- मंगल ग्रह (Mars)
- मंगल टोही परिक्रमा यान (Mars Reconnaissance Orbiter)
- मंदाकिनी (Milky way)
- मिरैन्डा (उपग्रह) (Miranda (moon))
- मित्रक तारा (Alpha Centauri)
- मुख्य अनुक्रम (Main sequence)
- लग्रांज बिन्दु (Lagrangian point)
- लाल बौना (Red dwarf)
- लाल महादानव तारा (Red supergiant)
- लाल बौना (Red dwarf)
- लेंसनुमा आकाशगंगा (Lenticular galaxy)
- लंबन (Parallax)
- वरुण (ग्रह) (Neptune)
- वरुण-पार वस्तुएँ (Trans-Neptunian object)
- वशिष्ठ और अरुंधती तारे (Mizar and Alcor)
- वासयोग्य क्षेत्र (Habitable zone)
- वेधशाला (Observatory)
- वियुति (opposition)
- विलियम हरशॅल (William Herschel)
- विषुव (Equinox)
- वॉयेजर द्वितीय (Voyager 2)
- वॉयेजर प्रथम (Voyager 1)
- वृष तारामंडल (Taurus (constellation))
- वृषपर्वा तारामंडल (Cepheus (constellation))
- व्याध तारा (Sirius)
- रिया (उपग्रह) (Rhea (moon))
- रोश सीमा (Roche limit)
- रोहिणी तारा (Aldebaran)
- यम (Pluto)
- यम के प्राकृतिक उपग्रह (Moons of Pluto)
- याम्योत्तर गमन (Culmination)
- यूरोपा (उपग्रह) (Europa (moon))
- युति (Conjunction)
- युलीसेस (Ulysses)
- यूरोपीय अंतरिक्ष अभिकरण (European Space Agency)
- शनि (Saturn)
- शनि के छल्ले (Rings of Saturn)
- शर्मिष्ठा तारामंडल (Cassiopeia (constellation))
- शिकारी तारामंडल (Orion (constellation))
- शिशुमार तारामंडल (Draco (constellation))
- शुक्र (Venus)
- सफ़ेद बौना (White dwarf)
- सर्पिल आकाशगंगा (Spiral Galaxy)
- सप्तर्षि मण्डल (Ursa Major)
- सामान्य सापेक्षता (General relativity)
- सापेक्ष कांतिमान (Apparent magnitude)
- स्थानीय समूह (Local group)
- स्थिति कोण (खगोलविज्ञान) (Phase angle)
- सीरीस (बौना ग्रह) (Ceres (dwarf planet))
- सूर्य (Sun)
- सूर्य ग्रहण (Solar eclipse)
- सूर्यपथ (Ecliptic)
- सूर्योच्य (Aphelion)
- सुब्रह्मण्यन् चन्द्रशेखर (Subrahmanyan Chandrasekhar)
- सुपरनोवा (Supernova)
- सौर द्रव्यमान (Solar mass)
- सौर मंडल (Solar System)
- सौर मण्डल की छोटी वस्तुएँ (Small Solar System body)
- सौर वायु (Solar wind)
- श्रवण तारा (Altair)
- हबल अनुक्रम (Hubble sequence)
- हबल अंतरिक्ष दूरदर्शी (Hubble Space Telescope)
- हउमेया (बौना ग्रह) (Haumea (dwarf planet))
- हाएड्रा (उपग्रह) (Hydra (moon))
- हेल-बॉप धूमकेतु (Comet Hale-Bopp)
- हेलियोस्फीयर (Heliosphere)
- हिप्पारकस (Hipparchus)
- हैली धूमकेतू (Halley’s Comet)
- होहमान्न स्थानांतरण कक्षा (Hohmann transfer orbit)
- हंस तारामंडल (Cygnus (constellation))
भारतीय आर्यो में ज्योतिष विद्या का ज्ञान अत्यन्त प्राचीन काल से था । यज्ञों की तिथि आदि निश्चित करने में इस विद्या का प्रयोजन पड़ता था । अयन चलन के क्रम का पता बराबर वैदिक ग्रंथों में मिलता है । जैसे, पुनर्वसु से मृगशिरा (ऋगवेद), मृगशिरा से रोहिणी (ऐतरेय ब्राह्मण), रोहिणी से कृत्तिका (तौत्तिरीय संहिता) कृत्तिका से भरणी (वेदाङ्ग ज्योतिष) । तैत्तरिय संहिता से पता चलता है कि प्राचीन काल में वासंत विषुवद्दिन कृत्तिका नक्षत्र में पड़ता था । इसी वासंत विषुवद्दिन से वैदिक वर्ष का आरम्भ माना जाता था, पर अयन की गणना माघ मास से होती थी । इसके बाद वर्ष की गणना शारद विषुवद्दिन से आरम्भ हुई । ये दोनों प्रकार की गणनाएँ वैदिक ग्रंथों में पाई जाती हैं । वैदिक काल में कभी वासंत विषुवद्दिन मृगशिरा नक्षत्र में भी पड़ता था । इसे बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद से अनेक प्रमाण देकर सिद्ध किया है । कुछ लोगों ने निश्चित किया है कि वासंत विषुबद्दिन की यह स्थिति ईसा से ४००० वर्ष पहले थी । अतः इसमें कोई संदेह नहीं कि ईसा से पाँच छह हजार वर्ष पहले हिंदुओं को नक्षत्र अयन आदि का ज्ञान था और वे यज्ञों के लिये पत्रा बनाते थे। शारद वर्ष के प्रथम मास का नाम अग्रहायण था जिसकी पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र में पड़ती थी । इसी से कृष्ण ने गीता में कहा है कि ‘महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ’ ।
प्राचीन हिंदुओं ने ध्रुव का पता भी अत्यन्त प्राचीन काल में लगाया था । अयन चलन का सिद्धान्त भारतीय ज्योतिषियों ने किसी दूसरे देश से नहीं लिया; क्योंकि इसके संबंध में जब कि युरोप में विवाद था, उसके सात आठ सौ वर्ष पहले ही भारतवासियों ने इसकी गति आदि का निरूपण किया था। वराहमिहिर के समय में ज्योतिष के सम्बन्ध में पाँच प्रकार के सिद्धांत इस देश में प्रचलित थे – सौर, पैतामह, वासिष्ठ, पौलिश ओर रोमक। सौर सिद्धान्त संबंधी सूर्यसिद्धान्त नामक ग्रंथ किसी और प्राचीन ग्रंथ के आधार पर प्रणीत जान पड़ता है। वराहमिहिर और ब्रह्मगुप्त दोनों ने इस ग्रंथ से सहायता ली है। इन सिद्धांत ग्रंथों में ग्रहों के भुजांश, स्थान, युति, उदय, अस्त आदि जानने की क्रियाएँ सविस्तर दी गई हैं । अक्षांश और देशातंर का भी विचार है।
पूर्व काल में देशान्तर लंका या उज्जयिनी से लिया जाता था । भारतीय ज्योतिषी गणना के लिये पृथ्वी को ही केंद्र मानकर चलते थे और ग्रहों की स्पष्ट स्थिति या गति लेते थे । इससे ग्रहों की कक्षा आदि के संबंध में उनकी और आज की गणना में कुछ अन्तर पड़ता है । क्रांतिवृत्त पहले २८ नक्षत्रों में ही विभक्त किया गया था । राशियों का विभाग पीछे से हुआ है । वैदिक ग्रंथों में राशियों के नाम नहीं पाए जाते । इन राशियों का यज्ञों से भी कोई संबंध नहीं हैं । बहुत से विद्वानों का मत है कि राशियों और दिनों के नाम यवन (युनानियों के) संपर्क के पीछे के हैं । अनेक पारिभाषिक शब्द भी यूनानियों से लिए हुए हैं, जैसे,— होरा, दृक्काण केंद्र, इत्यादि।
भारतीय ज्योतिष
भारतीय ज्योतिष ग्रहनक्षत्रों की गणना की वह पद्धति है जिसका भारत में विकास हुआ है। आजकल भी भारत में इसी पद्धति से पंचांग बनते हैं, जिनके आधार पर देश भर में धार्मिक कृत्य तथा पर्व मनाए जाते हैं। वर्तमान काल में अधिकांश पंचांग सूर्यसिद्धांत, मकरंद सारणियों तथा ग्रहलाघव की विधि से प्रस्तुत किए जाते हैं। कुछ ऐसे भी पंचांग बनते हैं जिन्हें नॉटिकल अल्मनाक के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, किन्तु इन्हें प्रायः भारतीय निर्णय पद्धति के अनुकूल बना दिया जाता है।
प्राचीन भारत में ज्योतिष का अर्थ ग्रहों और नक्षत्रों की चाल का अध्ययन करने के लिए था, यानि ब्रह्माण्ड के बारे में अध्ययन। कालान्तर में फलित ज्योतिष के समावेश के चलते ज्योतिष शब्द के मायने बदल गए और अब इसे लोगों का भाग्य देखने वाली विद्या समझा जाता है।
भारत का प्राचीनतम उपलब्ध साहित्य वैदिक साहित्य है। वैदिककाल के भारतीय यज्ञ किया करते थे। यज्ञों के विशिष्ट फल प्राप्त करने के लिये उन्हें निर्धारित समय पर करना आवश्यक था इसलिए वैदिककाल से ही भारतीयों ने वेधों द्वारा सूर्य और चंद्रमा की स्थितियों से काल का ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। पंचांग सुधारसमिति के अनुसार ऋग्वेद काल के आर्यों ने चांद्र-सौर वर्षगणना पद्धति का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वे १२ चांद्र मास तथा चांद्र मासों को सौर वर्ष से संबद्ध करनेवाले अधिमास को भी जानते थे। दिन को चंद्रमा के नक्षत्र से व्यक्त करते थे। उन्हें चंद्रगतियों के ज्ञानोपयोगी चांद्र राशिचक्र का ज्ञान था। वर्ष के दिनों की संख्या ३६६ थी, जिनमें से चांद्र वर्ष के लिये १२ दिन घटा देते थे। रिपोर्ट के अनुसार ऋग्वेदकालीन आर्यों का समय कम से कम १,२०० वर्ष ईसा पूर्व अवश्य होना चाहिए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की ओरायन के अनुसार यह समय शक संवत् से लगभग ४,००० वर्ष पहले ठहरता है।
यजुर्वेद काल में भारतीयों ने मासों के १२ नाम मधु, माधव, शुक्र, शुचि, नमस्, नमस्य, इष, ऊर्ज, सहस्र, तपस् तथा तपस्य रखे थे। बाद में यही पूर्णिमा में चन्द्रमा के नक्षत्र के आधार पर चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ तथा फाल्गुन हो गए। यजुर्वेद में नक्षत्रों की पूरी संख्या तथा उनकी अधिष्टात्री देवताओं के नाम भी मिलते हैं। यजुर्वेद में तिथि तथा पक्षों, उत्तर तथा दक्षिण अयन और विषुव दिन की भी कल्पना है। विषुव दिन वह है जिस दिन सूर्य विषुवत् तथा क्रांतिवृत्त के संपात में रहता है। श्री शंकर बालकृष्ण दीक्षित के अनुसार यजुर्वेदकाल के आर्यों को गुरु, शुक्र तथा राहु-केतु का ज्ञान था। यजुर्वेद के रचनाकाल के विषय में विद्वानों में मतभेद है। यदि हम पाश्चात्य पक्षपाती, कीथ का मत भी लें तो यजुर्वेद की रचना ६०० वर्ष ईसा पूर्व हो चुकी थी। इसके पश्चात् वेदांग ज्योतिष का काल आता है, जो ईसा पूर्व १,४०० वर्षों से लेकर ईसा पूर्व ४०० वर्ष तक है। वेदांग ज्योतिष के अनुसार पाँच वर्षों का युग माना गया है, जिसमें १८३० माध्य सावन दिन, ६२ चांद्र मास, १८६० तिथियाँ तथा ६७ नाक्षत्र मास होते हैं। युग के पाँच वर्षों के नाम हैं.. संवत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर तथा इद्ववत्सर। इसके अनुसार तिथि तथा चांद्र नक्षत्र की गणना होती थी। इसके अनुसार मासों के माध्य सावन दिनों की गणना भी की गई है। वेदांङ्ग ज्यातिष में जो हमें महत्वपूर्ण बात मिलती है वह युग की कल्पना, जिसमें सूर्य और चंद्रमा के प्रत्यक्ष वेधों के आधार पर मध्यम गति ज्ञात करके इष्ट तिथि आदि निकाली गई है। आगे आनेवाले सिद्धांत ज्योतिष के ग्रंथों में इसी प्रणाली को अपनाकर मध्यम ग्रह निकाले गए हैं।
सिद्धान्त ज्योतिष प्रणाली से लिखा हुआ प्रथम पौरुष ग्रंथ आर्यभट प्रथम की आर्यभटीयम् (शक संo ४२१) है। तत्पश्चात् बराहमिहिर (शक संo ४२७) द्वारा संपादित सिद्धांतपंचिका है, जिसमें पितामह, वासिष्ठ, रोमक, पुलिश तथा सूर्यसिद्धांतों का संग्रह है। इससे यह तो पता चलता है कि बराहमिहिर से पूर्व ये सिद्धांतग्रंथ प्रचलित थे, किंतु इनके निर्माणकाल का कोई निर्देश नहीं है। सामान्यतः भारतीय ज्योतिष ग्रंथकारों ने इन्हें अपौरुषेय माना है। आधुनिक विद्वानों ने अनुमानों से इनके कालों को निकाला है और ये परस्पर भिन्न हैं। इतना निश्चित है कि ये वेदांग ज्योतिष तथा बराहमिहिर के समय के भीतर प्रचलित हो चुके थे। इसके बाद लिखे गए सिद्धांतग्रंथों में मुख्य हैं : ब्रह्मगुप्त (शक संo ५२०) का ब्राह्मस्फुटसिद्धान्त, लल्ल (शक संo ५६०) का शिष्यधीवृद्धिद, श्रीपति (शक संo ९६१) का सिद्धान्तशेखर, भास्कराचार्य (शक संo १०३६) का सिद्धान्तशिरोमणि, गणेश (१४२० शक संo) का ग्रहलाघव तथा कमलाकर भट्ट (शक संo १५३०) का सिद्धांत-तत्व-विवेक।
गणित ज्योतिष के ग्रंथों के दो वर्गीकरण हैं : सिद्धान्त ग्रन्थ तथा करण ग्रंथ। सिद्धांतग्रंथ युगादि अथवा कल्पादि पद्धति से तथा करणग्रंथ किसी शक के आरंभ की गणनापद्धति से लिखे गए हैं। गणित ज्योतिष ग्रंथों के मुख्य प्रतिपाद्य विषय है: मध्यम ग्रहों की गणना, स्पष्ट ग्रहों की गणना, दिक्, देश तथा काल, सूर्य और चंद्रगहण, ग्रहयुति, ग्रहच्छाया, सूर्य सांनिध्य से ग्रहों का उदयास्त, चंद्रमा की शृंगोन्नति, पातविवेचन तथा वेधयंत्रों का विवेचन।
भारतीय ज्योतिष → गणना प्रणाली
पूरे वृत्त की परिधि ३६० मान ली जाती है। इसका ३६० वाँ भाग एक अंश, उसका ६०वाँ भाग एक कला, कला का ६०वाँ भाग एक विकला, एक विकला का ६०वाँ भाग एक प्रतिविकला होता है। ३० अंश की एक राशि होती है। ग्रहों की गणना के लिये क्रांतिवृत्त के, जिसमें सूर्य भ्रमण करता दिखलाई देता है, १२भाग माने जाते हैं। इन भागों को मेष, वृष आदि राशियों के नाम से पुकारा जाता है। ग्रह की स्थिति बतलाने के लिये मेषादि से लेकर ग्रह के राशि, अंग, कला, तथा विकला बता दिए जाते हैं। यह ग्रह का भोगांश होता है। सिद्धांत ग्रंथों में प्रायः एक वृत्तचतुर्थांश (९०अंश का चाप) के २४ भाग करके उसकी ज्याएँ तथा कोटिज्याएँ निकाली रहती है। इनका मान कलात्मक रहता है। ९० के चाप की ज्या वृहद्वृत्त का अर्धव्यास होती है, जिसे त्रिज्या कहते हैं। इसको निम्नलिखित सूत्र से निकालते हैं :
परिधि = (३९२७ / १२५०) x व्यास
भारतीय ज्योतिष → कालगणना
विषुवद् वृत्त में एक समगति से चलनेवाले मध्यम सूर्य (लंकोदयासन्न) के एक उदय से दूसरे उदय तक एक मध्यम सावन दिन होता है। यह वर्तमान कालिक अंग्रेजी के ‘सिविल डे’ जैसा है। एक सावन दिन में ६० घटी; १ घटी २४ मिनिट साठ पल; १ पल २४ सेंकेड ६० विपल तथा ढाई विपल १ सेंकेंड होते हैं। सूर्य के किसी स्थिर बिंदु (नक्षत्र) के सापेक्ष पृथ्वी की परिक्रमा के काल को सौर वर्ष कहते हैं। यह स्थिर बिंदु मेषादि है। ईसा के पाँचवे शतक के आसन्न तक यह बिंदु कांतिवृत्त तथा विषुवत् के संपात में था। अब यह उस स्थान से लगभग २३ पश्चिम हट गया है, जिसे अयनांश कहते हैं। अयनगति विभिन्न ग्रंथों में एक सी नहीं है। यह लगभग प्रति वर्ष १ कला मानी गई है। वर्तमान सूक्ष्म अयनगति ५०.२ विकला है। सिद्धांतग्रथों का वर्षमान ३६५ दिo १५ घo ३१ पo ३१ विo २४ प्रति विo है। यह वास्तव मान से ८। ३४। ३७ पलादि अधिक है। इतने समय में सूर्य की गति ८.२७” होती है। इस प्रकार हमारे वर्षमान के कारण ही अयनगति की अधिक कल्पना है। वर्षों की गणना के लिये सौर वर्ष का प्रयोग किया जाता है। मासगणना के लिये चांद्र मासों का। सूर्य और चंद्रमा जब राश्यादि में समान होते हैं तब वह अमांतकाल तथा जब ६ राशि के अंतर पर होते हैं तब वह पूर्णिमांतकाल कहलाता है। एक अमांत से दूसरे अमांत तक एक चांद्र मास होता है, किंतु शर्त यह है कि उस समय में सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में अवश्य आ जाय। जिस चांद्र मास में सूर्य की संक्रांति नहीं पड़ती वह अधिमास कहलाता है। ऐसे वर्ष में १२ के स्थान पर १३ मास हो जाते हैं। इसी प्रकार यदि किसी चांद्र मास में दो संक्रांतियाँ पड़ जायँ तो एक मास का क्षय हो जाएगा। इस प्रकार मापों के चांद्र रहने पर भी यह प्रणाली सौर प्रणाली से संबद्ध है। चांद्र दिन की इकाई को तिथि कहते हैं। यह सूर्य और चंद्र के अंतर के १२वें भाग के बराबर होती है। हमारे धार्मिक दिन तिथियों से संबद्ध है १ चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है उसे चांद्र नक्षत्र कहते हैं। अति प्राचीन काल में वार के स्थान पर चांद्र नक्षत्रों का प्रयोग होता था। काल के बड़े मानों को व्यक्त करने के लिये युग प्रणाली अपनाई जाती है। वह इस प्रकार है:
- कृतयुग (सत्ययुग) १७,२८,००० वर्ष
- द्वापर १२,९६,००० वर्ष
- त्रेता ८, ६४,००० वर्ष
- कलि ४,३२,००० वर्ष
- योग महायुग ४३,२०,००० वर्ष
- कल्प १,००० महायुग ४,३२,००,००,००० वर्ष
सूर्य सिद्धांत में बताए आँकड़ों के अनुसार कलियुग का आरंभ १७ फ़रवरी ३१०२ ईo पूo को हुआ था। युग से अहर्गण (दिनसमूहों) की गणना प्रणाली, जूलियन डे नंबर के दिनों के समान, भूत और भविष्य की सभी तिथियों की गणना में सहायक हो सकती है।
भारतीय ज्योतिष → (मध्य ग्रह गणना)
ग्रह की मेषादि के सापेक्ष पृथ्वी की परिक्रमा को एक भगण कहते हैं। सिद्धांत ग्रथों में युग, या कल्पग्रहों, के मध्य भगण दिए रहते हैं। युग या कल्प के मध्य सावन दिनों की संख्या भी दी रहती है। यदि युग या कल्प के प्रारंभ में ग्रह मेषादि में हों तो बीच के दिन (अहर्गण) ज्ञात होने से मध्यम ग्रह को त्रैराशिक से निकाला जा सकता है। भगण की परिभाषा के अनुसार बुध और शुक्र की मध्यम गति सूर्य के समान ही मानी गई है। उनकी वास्तविक गति के तुल्य उनकी शीघ्रोच्च गति मानी गई है। ये ग्रह रेखादेश, अर्थात् उज्जयिनी, के याम्योत्तर के आते हैं, जिन्हें देशांतर तथा चर संस्कारों से अपने स्थान के मयम सर्योदयासन्नकालिक बनाया जाता है।
भारतीय ज्योतिष → (मंद स्पष्ट ग्रह)
स्पष्ट सूर्य और चंद्रमा की स्पष्ट गति जिस समय सबसे कम हो उस समय के स्पष्ट सूर्य और चंद्रमा का जितना भाग होगा उसे उनके मंदोच्च का भोग समझना चाहिए। स्पष्ट रवि चंद्र और मध्यम रवि चंद्र के अंतर को मंदफल कहते हैं। मंदोच्च से १८० की दूरी पर मंदनीच होगा। मंदोच्च से छह राशि तक स्पष्ट सूर्य चंद्र मध्यम सूर्य चंद्र से पीछे रहते हैं। इसलिये मंद फल ऋण होता है। मंदोच्च से मध्यम ग्रह के अंतर की मंदकेंद्र संज्ञा है। मंदोच्च से ३ राशि के अंतर पर मंदफल परमार्धिक होता है। उसे मंदांत्य फल कहते हैं। मंदनीच से मंदोच्च तक स्पष्ट ग्रह मध्यम ग्रह से आगे रहता है, अतः मंदफल धन होता है। मंदस्पष्ट रवि चंद्र के मंदफल को ज्ञात करने के लिये दो प्रकार के क्षेत्रों की कल्पना है, जिन्हें भंगि कहते हैं। पहली का नाम प्रतिवृत्त भंगि है। भू को केंद्र मानकर एक त्रिज्या के व्यासार्ध से वृत्त खींचा, वह कक्षावृत्त हुआ। इसके ऊर्ध्वाधरव्यास पर मंद अत्यफल की ज्या के तुल्य काटकर उस केंद्र से एक त्रिज्या व्यास से वृत्त खींचा वह मंदप्रतिवृत्त होगा। मध्यम ग्रह को मंदप्रतिवृत्त में चलता कल्पित किया। यदि कक्षा वृत्त में भी मंदकेंद्र के तुल्य चाप काटें तो वहाँ कक्षावृत्त का मध्यम ग्रह होगा। भूकेंद्र से प्रतिवृत्त स्थित ग्रह तक खींची गई रेखा कक्षावृत्त में जहॉ लगे वह मंदस्पष्ट ग्रह होगा। कक्षावृत्त के मध्यम और मंदस्पष्ट ग्रह का अंतर मंदफल होगा। नीचोच्च भंगि के लिये कक्षावृत्त पर स्थित मध्यम ग्रह से मंदांत्यफलज्या तुल्य व्यासार्ध से एक वृत्त खींच लेते हैं, जिसे मंदपरिधि वृत्त कहते हैं। कक्षावृत्त के केंद्र से मध्यम ग्रह से जाती हुई रेखा जहाँ मंदपरिधिवृत्त में लगे उसे मंदोच्च मानकर, मंद परिधि में विपरीत दिशा में, केंद्र के तुल्य अंशों पर ग्रह की कल्पना की जाती है। ग्रह से भूकेंद्र को मिलानेवाली रेखा (मंदकर्ण) जिस स्थान पर कक्षावृत्त को काटे वहाँ मंदस्पष्ट ग्रह होगा। इस प्रकार मंदस्पष्ट किए गए सूर्य और चंद्र हमें उन स्थानों पर दिखलाई देते हैं, क्योंकि उनका भ्रमण हमें पृथ्वीकेंद्र के सापेक्ष दिखलाई पड़ता है। शेष ग्रहों के लिये भी मंदफल निकालने की वैसी ही कल्पना है। उनका मंदोच्च स्पष्ट ग्रह से विलोमरीति द्वारा मंदस्पष्ट का ज्ञान करके ज्ञात करते हैं। ये मंदस्पष्ट ग्रह दृश्य नहीं होते, क्योंकि पृथ्वी उनके भ्रमण का केंद्र नहीं है। ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि मंदस्पष्ट ग्रह अपनी कक्षा में घूमते ग्रह का भोग होता है। अतएव भूदृश्य बनाने के लिये पाँच ग्रहों के लिये शीघ्र फल की कल्पना की गई है।
भारतीय ज्योतिष → ( स्पष्ट ग्रह)
मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, तथा शनि को स्पष्ट करने के लिये शीघ्रफल की कल्पना है। इसके लिये भी मंद प्रतिवृत्त तथा मंदनीचोच्च जैसी भंगियों की कल्पना की जाती है, जिसके लिये मंद के स्थान पर शीघ्र शब्द रख दिया जाता है। अंतर्ग्रहों के लिये वास्तविक मध्यमग्रहों को ही शीघ्रोच्च कहते हैं। उनके माध्य अधिकतम रविग्रहांतर कोण को परमशीघ्रफल, परमशीघ्रफल की ज्या को शीघ्रांत्य फलज्या कहते हैं। ग्रह (मध्यमरवि) और शीघ्रोच्च का अंतर शीघ्रकेंद्र होता है। इसमें मंदफल के लिये बनाई गई भंगियों की तरह भंगियाँ बनाकर शीघ्रफल निकाला जाता है। इस प्रकार के संस्कार से ग्रह का इष्ट रविग्रहांतर कोण करके ग्रह की स्थिति ज्ञात हो जाती है। बहिर्ग्रहों के लिये रविकेंद्रिक परमलंबन की परमशीघ्रफल तथा रवि को शीघ्रोच्च मानकर शीघ्रफल ज्ञात किया जाता है। शीघ्रफल के संस्कार की विधि आचार्यों ने इस प्रकार निर्द्धारित की है कि उपलब्ध ग्रह का भोग यथार्थ आ सके।
भारतीय ज्योतिष → (ग्रहों की कक्षाएँ)
ग्रहों की कक्षाएँ चंद्र, बुध, शुक्र, रवि, भौम, गुरु, शनि के क्रम से उत्तरोत्तर पृथ्वी से दूर हैं। इनका केंद्र पृथ्वी माना गया है यद्यपि ग्रहों के साधन के लिये प्रत्येक कक्षा का अर्धव्यास त्रिज्यातुल्य कल्पित किया है, तथापि उनकी अंत्यफलज्या भिन्न होने के कारण उनकी दूरी विभिन्न प्रकार की आती है। शीघ्रांत्यफलज्याओं और त्रिज्याओं की ग्रहकक्षाव्यासार्धं और रविकक्षाव्यासार्ध से तुलना करने पर बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति तथा शनि की कक्षाओं के व्यासार्ध पृथ्वी से रवि की दूरी के सापेक्ष .३६९४, .७२७८, १.५१३९, ५.१४२९ तथा ९.२३०८ आते हैं। आधुनिक सूक्ष्म मान .३८७१, .७२३३, १.५२३७, ५.२०२८ तथा ९.५२८८ हैं। ग्रहकक्षा और क्रांतिवृत्त के संपात को पात कहते हैं। ग्रह के भ्रमणमार्ग को विमंडल कहते हैं। क्रांतिवृत्त तथा विमंडल के बीच के कोण को परमविक्षेप कहते हैं। इनके मान भूकेंद्रिक ज्ञात किए गए हैं। तमोग्रह राहु केतु सदा चंद्रमा के पातों पर कल्पित किए जाते हैं। पात की गति विलोम होती है।
ग्रहणाधिकारों में सूर्य तथा चंद्र के ग्रहणों का गणित है। चंद्रमा का ग्रहण भूछाया में प्रविष्ट होने से तथा सूर्यग्रहण चंद्रमा द्वारा सूर्य के ढके जाने से माना गया है। सूर्यग्रहण में लंबन के कारण भूकेंद्रीय चंद्र तथा हमें दिखाई देनेवोल चंद्र में बहुत अंतर आ जाता है। अत: इसके लिये लंबन का ज्ञान किया जाता है।
चंद्रशृंगोन्नति में चंद्रमा की कलाओं को ज्ञात किया जाता है। ग्रहच्छायाधिकार में ग्रहों के उदयास्त काल तथा इष्टकाल में वेध की विधि और पाताधिकार में सूर्य और चंद्रमा के क्रांतिसाम्य का विचार किया जाता है। भिन्न अयन तथा एक गोलार्ध में होने पर, सायन रिवचंद्र के योग १८०° के समय क्रांतिसाम्य होने पर, व्यतिपात तथा एक अयन भिन्न गोलार्ध में होने पर वही योग ३६०° के तुल्य हो तो क्रांतिसाम्य में वैधृति होती है। ये दोनों शुभ कार्यों के लिये वर्जित हैं। ग्रहयुति में ग्रहों के अति सान्निध्य की स्थितियों का (युद्ध समागम का) गणित है। भग्रहयुति में नक्षत्रों के नियामक दिए गए हैं।
भारतीय ज्योतिष प्रणाली से बनाए तिथिपत्र को पंचांग कहते हैं। पंचांग के पाँच अंग हैं : तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा करण। पंचांग में इनके अतिरिक्त दैनिक, दैनिक लग्नस्पष्ट, ग्रहचार, ग्रहों के सूर्यसान्निध्य से उदय और अस्त और चंद्रोदयास्त दिए रहते हैं। इनके अतिरिक्त इनमें विविध मुहूर्त तथा धार्मिक पर्व दिए रहते हैं।
भारतीय ज्योतिष → पञ्चाङ्ग
हिन्दू पञ्चाङ्ग से आशय उन सभी प्रकार के पञ्चाङ्गों से है जो परम्परागत रूप प्राचीन काल से भारत में प्रयुक्त होते आ रहे हैं। पंचांग शब्द का अर्थ है , पाँच अंगो वाला। पंचांग में समय गणना के पाँच अंग हैं : वार , तिथि , नक्षत्र , योग , और करण। ये चान्द्रसौर प्रकृति के होते हैं। सभी हिन्दू पञ्चाङ्ग, कालगणना के एक समान सिद्धांतों और विधियों पर आधारित होते हैं किन्तु मासों के नाम, वर्ष का आरम्भ (वर्षप्रतिपदा) आदि की दृष्टि से अलग होते हैं।भारत में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख पञ्चाङ्ग ये हैं-
- (१) विक्रमी पञ्चाङ्ग – यह सर्वाधिक प्रसिद्ध पञ्चाङ्ग है जो भारत के उत्तरी, पश्चिमी और मध्य भाग में प्रचलित है।
- (२) तमिल पञ्चाङ्ग – दक्षिण भारत में प्रचलित है,
- (३) बंगाली पञ्चाङ्ग – बंगाल तथा कुछ अन्य पूर्वी भागों में प्रचलित है।
- (४) मलयालम पञ्चाङ्ग – यह केरल में प्रचलित है और सौर पंचाग है।
हिन्दू पञ्चाङ्ग का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल से होता आ रहा है और आज भी भारत और नेपाल सहित कम्बोडिया, लाओस, थाईलैण्ड, बर्मा, श्री लंका आदि में भी प्रयुक्त होता है। हिन्दू पञ्चाङ्ग के अनुसार ही हिन्दुओं/बौद्धों/जैनों/सिखों के त्यौहार होली, गणेश चतुर्थी, सरस्वती पूजा, महाशिवरात्रि, वैशाखी, रक्षा बन्धन, पोंगल, ओणम ,रथ यात्रा, नवरात्रि, लक्ष्मी पूजा, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, रामनवमी, विसु और दीपावली आदि मनाए जाते हैं।
भारतीय ज्योतिष → वार, सप्ताह के दिन
भारतीय पंचांग प्रणाली में एक प्राकृतिक सौर दिन को सावन दिवस कहा जाता है। सप्ताह में सात दिन होते हैं और उनको वार कहा जाता है। दिनों के नाम सूर्य , चन्द्र , और पांच प्रमुख ग्रहों पर आधारित हैं , जैसे नाम यूरोप में भी प्रचलित हैं।
- १. रविवासर आदित्य वासरर, विवार (आइत्तवार ,इत्तवार,इतवार अतवार , एतवार) सूर्य, Sunday/dies Solis.
- २. सोमवासर, सोमवार (सुम्मार), चन्द्र, Monday/dies Lunae.
- ३. मङ्गलवासर या भौम वासर, मंगलवार (मंगल), मंगल, Tuesday/dies Martis.
- ४. बुधवासर या सौम्य वासर, बुधवार, (बुध), बुध, Wednesday/dies Mercurii.
- ५. गुरुवासर, बृहस्पतिवासर, गुरुवार, बृहस्पतिवार (बृहस्पत), बृहस्पति/गुरु, Thursday/dies Jupiter.
- ६. शुक्रवासर शुक्रवार, (सुक्कर), शुक्र, Friday/dies Veneris.
- ७. शनिवासर, शनिवार, (थावर, शनिचर, सनीच्चर), शनि, Saturday/dies Saturnis.
भारतीय ज्योतिष → काल गणना – घटि , पल , विपल
हिन्दू समय गणना में समय की अलग अलग माप इस प्रकार हैं। एक सूर्यादय से दूसरे सूर्योदय तक का समय दिवस है , एक दिवस में एक दिन और एक रात होते हैं। दिवस से आरम्भ करके समय को साठ साठ के भागों में विभाजित करके उनके नाम रखे गए हैं ।
१ दिवस = ६० घटि (६० घटि २४ घंटे के बराबर है या १ घटी = २४ मिनट , घटि को देशज भाषा में घडी भी कहा जाता है )
१ घटी = ६० पल (६० पल २४ मिनट के बराबर है या १ पल = २४ सेकेण्ड)
१ पल = ६० विपल (६० विपल २४ सेकेण्ड के बराबर है , १ विपल = ०.४ सेकेण्ड)
१ विपल = ६० प्रतिविपल
इसके अतिरिक्त १ पल = ६ प्राण (१ प्राण = ४ सेकेण्ड)
इस प्रकार एक दिवस में ३६० पल होते हैं। एक दिवस में जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो उसके कारण सूर्य विपरीत दिशा में घूमता प्रतीत होता है। ३६० पलों में सूर्य एक चक्कर पूरा करता है , इस प्रकार ३६० पलों में ३६० अंश। १ पल में सूर्य का जितना कोण बदलता है उसे १ अंश कहते है।
भारतीय ज्योतिष → तिथि, पक्ष और माह
हिन्दू पंचांगों में मास, माह, या महीना चन्द्रमा के अनुसार होता है। अलग अलग दिन पृथ्वी से देखने पर चन्द्रमा के भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। जिस दिन चन्द्रमा पूरा दिखाई देता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के बाद चन्द्रमा घटने लगता है और अमावस्या तक घटता रहता है। अमावस्या के दिन चन्द्रमा दिखाई नहीं देता और फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और लगभग चौदह या पन्द्रह दिनों में बढ़कर पूरा हो जाता है। इस प्रकार चन्द्रमा के चक्र के दो भाग है। एक भाग में चन्द्रमा पूर्णिमा के बाद से अमावस्या तक घटता है , इस भाग को ‘कृष्ण पक्ष’ कहते हैं। इस पक्ष में रात के आरम्भ मे चाँदनी नहीं होती है। अमावस्या के बाद चन्द्रमा बढ़ने लगता है। अमावस्या से पूर्णिमा तक के समय को ‘शुक्ल पक्ष’ कहते हैं। पक्ष को साधारण भाषा में ‘पखवाड़ा’ भी कहा जाता है। चन्द्रमा का यह चक्र जो लगभग २९.५ दिनों का है ‘चंद्रमास’ या चन्द्रमा का महीना कहलाता है । दूसरे शब्दों में एक पूर्ण चन्द्रमा वाली स्थिति से अगली पूर्ण चन्द्रमा वाली स्थिति में २९.५ का अन्तर होता है।
चंद्रमास २९.५ दिवस का है , ये समय तीस दिवस से कुछ ही कम है। इस समय के तीसवें भाग को ‘तिथि’ कहते हैं। इस प्रकार एक तिथि एक दिन से कुछ मिनट कम होती है। पूर्ण चन्द्रमा की स्थिति (जिसमे स्थिति में चन्द्रमा सम्पूर्ण दिखाई देता हो ) आते ही पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाती है और कृष्ण पक्ष की पहली तिथि आरम्भ हो जाती है। दोनों पक्षों में तिथियाँ एक से चौदह तक बढ़ती हैं और पक्ष की अंतिम तिथि अर्थात पंद्रहवी तिथि पूर्णिमा या अमावस्या होती है।
तिथियों के नाम निम्न हैं- पूर्णिमा (पूरनमासी), प्रतिपदा (पड़वा), द्वितीया (दूज), तृतीया (तीज), चतुर्थी (चौथ), पंचमी (पंचमी), षष्ठी (छठ), सप्तमी (सातम), अष्टमी (आठम), नवमी (नौमी), दशमी (दसम), एकादशी (ग्यारस), द्वादशी (बारस), त्रयोदशी (तेरस), चतुर्दशी (चौदस) और अमावस्या (अमावस)।
माह के अंत के दो प्रचलन है। कुछ स्थानों पर पूर्णिमा से माह का अंत करते हैं और कुछ स्थानों पर अमावस्या से। पूर्णिमा से अंत होने वाले माह ‘पूर्णिमांत’ कहलाते हैं और अमावस्या से अंत होने वाले माह ‘अमावस्यांत’ कहलाते हैं। अधिकांश स्थानों पर पूर्णिमांत माह का ही प्रचलन है। चन्द्रमा के पूर्ण होने की सटीक स्थिति सामान्य दिन के बीच में भी हो सकती है और इस प्रकार अगली तिथि का आरम्भ दिन के बीच से ही सकता है।
भारतीय ज्योतिष → योग और करण
चन्द्रमा और सूर्य दोनों मिलकर जितने समय में एक नक्षत्र के बराबर दूरी (कोण) तय करते हैं उसे योग कहते हैं, क्योंकि ये चन्द्रमा और सूर्य की दूरी का योग है । ज्योतिष में ग्रहों की विशेष स्थितियों को भी योग कहा जाता है वह एक भिन्न विषय है। एक तिथि का आधा समय करण है।
भारतीय ज्योतिष → चन्द्रमास और ग्रहण
सूर्य और चंद्र ग्रहण का सम्बन्ध सूर्य और चन्द्रमा की पृथ्वी के सापेक्ष स्थितियों से है। सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या को ही आरम्भ होते है और चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही आरम्भ होते हैं। एक पूर्ण सूर्य ग्रहण की सहायता से अमावस्या तिथि के अंत को समझना सरल है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का आरम्भ अमावस्या तिथि में होता है , जब सूर्य ग्रहण पूर्ण होता है तब अमावस्या तिथि का अंत होता है और उसके बाद अगली तिथि आरम्भ हो जाती है जिसमे सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है। दो सूर्य ग्रहणों या दो चंद्र ग्रहणों के बीच का समय एक या छह चंद्रमास हो सकता हैं। ग्रहणों के समय का अध्ययन चंद्रमासों में करना सरल है क्योकि ग्रहणों के बीच की अवधि को चंद्रमासों में पूरा पूरा विभाजित किया जा सकता है
भारतीय ज्योतिष → महीनों के नाम
इन बारह मासों के नाम आकाशमण्डल के नक्षत्रों में से १२ नक्षत्रों के नामों पर रखे गये हैं। जिस मास जो नक्षत्र आकाश में प्रायः रात्रि के आरम्भ से अन्त तक दिखाई देता है या कह सकते हैं कि जिस मास की पूर्णमासी को चन्द्रमा जिस नक्षत्र में होता है, उसी के नाम पर उस मास का नाम रखा गया है। चित्रा नक्षत्र के नाम पर चैत्र मास (मार्च-अप्रैल), विशाखा नक्षत्र के नाम पर वैशाख मास (अप्रैल-मई), ज्येष्ठा नक्षत्र के नाम पर ज्येष्ठ मास (मई-जून), आषाढ़ा नक्षत्र के नाम पर आषाढ़ मास (जून-जुलाई), श्रवण नक्षत्र के नाम पर श्रावण मास (जुलाई-अगस्त), भाद्रपद (भाद्रा) नक्षत्र के नाम पर भाद्रपद मास (अगस्त-सितम्बर), अश्विनी के नाम पर आश्विन मास (सितम्बर-अक्टूबर), कृत्तिका के नाम पर कार्तिक मास (अक्टूबर-नवम्बर), मृगशीर्ष के नाम पर मार्गशीर्ष (नवम्बर-दिसम्बर), पुष्य के नाम पर पौष (दिसम्बर-जनवरी), मघा के नाम पर माघ (जनवरी-फरवरी) तथा फाल्गुनी नक्षत्र के नाम पर फाल्गुन मास (फरवरी-मार्च) का नामकरण हुआ है।
(१). चैत्र – चैत्र का महीना इस ब्रह्मांड का पहला दिन माना जाता है इसी महीने से होती है हिंदू नववर्ष की शुरूआत। जिसे संवत्सर कहा जाता है।
हिंदू वर्ष का पहला मास होने के कारण चैत्र की बहुत ही अधिक महता होती है। अनेक पावन पर्व इस मास में मनाये जाते हैं। चैत्र मास की पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में होती है इसी कारण इसका महीने का नाम चैत्र पड़ा।
मान्यता है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना आरंभ की थी। वहीं सतयुग की शुरुआत भी चैत्र माह से मानी जाती है।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी महीने की प्रतिपदा को भगवान विष्णु के दशावतारों में से पहले अवतार मतस्यावतार अवतरित हुए एवं जल प्रलय के बीच घिरे मनु को सुरक्षित स्थल पर पंहुचाया था। जिनसे प्रलय के पश्चात नई सृष्टि का आरंभ हुआ।
(२). वैशाख – वैशाख भारतीय काल गणना के अनुसार वर्ष का दूसरा माह है। इस माह को एक पवित्र माह के रूप में माना जाता है। जिनका संबंध देव अवतारों और धार्मिक परंपराओं से है। ऐसा माना जाता है कि इस माह के शुक्ल पक्ष को अक्षय तृतीया के दिन विष्णु अवतारों नर नारायण, परशुराम, नृसिंह और ह्ययग्रीव के अवतार हुआ और शुक्ल पक्ष की नवमी को देवी सीता धरती से प्रकट हुई। कुछ मान्यताओं के अनुसार त्रेतायुग की शुरुआत भी वैशाख माह से हुई। इस माह की पवित्रता और दिव्यता के कारण ही कालान्तर में वैशाख माह की तिथियों का सम्बंध लोक परंपराओं में अनेक देव मंदिरों के पट खोलने और महोत्सवों के मनाने के साथ जोड़ दिया। यही कारण है कि हिन्दू धर्म के चार धाम में से एक बद्रीनाथधाम के कपाट वैशाख माह की अक्षय तृतीया को खुलते हैं। इसी वैशाख के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को एक और हिन्दू तीर्थ धाम पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा भी निकलती है। वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या को देववृक्ष वट की पूजा की जाती है। यह भी माना जाता है कि भगवान बुद्ध की वैशाख पूजा ‘दत्थ गामणी’ (लगभग १००-७७ ई. पू.) नामक व्यक्ति ने लंका में प्रारम्भ करायी थी।
(३). ज्येष्ठ – ज्येष्ठ भारतीय काल गणना (हिन्दू पंचांग) के अनुसार वर्ष का तीसरा माह है। फागुन माह की विदाई के साथ ही गर्मी शुरू हो जाती है और इस माह को गर्मी का महीना भी कहा जाता है।
(४). आषाढ़ – हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह से प्रारंभ होने वाले वर्ष का चौथा महीना, जो ईस्वी कलेंडर के जून या जुलाई माह में पड़ता है। इसे वर्षा ऋतु का महीना भी कहा जाता है क्यों कि इस समय भारत में काफ़ी वर्षा होती है।
(५). श्रावण – श्रावण हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह से प्रारंभ होने वाले वर्ष का पांचवा महीना जो ईस्वी कलेंडर के जुलाई या अगस्त माह में पड़ता है। इसे वर्षा ऋतु का महीना भी कहा जाता है क्यों कि इस समय भारत में अत्यधिक वर्षा होती है।
श्रावण मास शिवजी को विशेष प्रिय है, भोलेनाथ ने स्वयं कहा है—
द्वादशस्वपि मासेषु श्रावणो मेऽतिवल्लभः।
श्रवणार्हं यन्माहात्म्यं तेनासौ श्रवणो मतः ॥
श्रवणर्क्षं पौर्णमास्यां ततोऽपि श्रावण: स्मृतः।
यस्य श्रवणमात्रेण सिद्धिद: श्रावणोऽप्यतः ॥
अर्थात मासों में श्रावण मुझे अत्यंत प्रिय है। इसका माहात्म्य सुनने योग्य है अतः इसे श्रावण कहा जाता है। इस मास में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है इस कारण भी इसे श्रावण कहा जाता है। इसके माहात्म्य के श्रवण मात्र से यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है।
(६). भाद्रपद – भारतीय काल गणना के अनुसार साल का छटवा माह जो अगस्त के महीने में पड़ता है। इस समय भारत में वर्षा की ऋतु होती है।
(७). आश्विन – भारतीय काल गणना के अनुसार साल का सातवां महीनि आश्विन है।
(८). कार्तिक – भारतीय काल गणना के अनुसार साल का आठवां महीना कार्तिक है।
(९). अगहन – हिन्दू वर्ष का नवां महीना अगहन अथवा अग्रहायण के नाम से जाना जाता है। इसका प्रचलित नाम मार्गशीर्ष एवं मगसर हैं।
(१०). पौष – हिन्दू पंचांग के अनुसार साल के दसवें माह का नाम पौष हैं। इस मास में हेमंत ऋतु होने से ठंड अधिक होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस मास में भग नाम सूर्य की उपासना करना चाहिए।
(११). माघ – माघ हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष का ग्यारहवाँ महीना है।
(१२). फाल्गुन – फाल्गुन का महीना हिन्दू पंचांग का अंतिम महीना है. इस महीने की पूर्णिमा को फाल्गुनी नक्षत्र होने के कारण इस महीने का नाम फाल्गुन है. इस महीने को आनंद और उल्लास का महीना कहा जाता है. इस महीने से धीरे धीरे गरमी की शुरुआत होती है,और सर्दी कम होने लगती है।
भारतीय ज्योतिष → सम्वत्
आमतौर पर प्रचलित भारतीय वर्ष गणना प्रणालियों में प्रत्येक को सम्वत कहा जाता है। हिन्दू , बौद्ध , और जैन परम्पराओं में कई सम्वत प्रचलित हैं जिसमे विक्रमी सम्वत , शक सम्वत , प्राचीन शक सम्वत प्रसिद्द हैं।
अन्य संम्वत्
- प्राचीन सप्तर्षि ६६७६ ईपू
- कलियुग संवत् ३१०२ ईपू
- सप्तर्षि संवत ३०७६ ईपू
- वीर निर्वाण संवत
- शक संवत ७८ ई.
- कल्चुरी संवत २४८ ई.
सम्वत या तो कार्तिक शुल्क पक्ष से आरम्भ होते हैं या चैत्र शुक्ल पक्ष से। कार्तिक से आरम्भ होने वाले सम्वत को कर्तक सम्वत कहते हैं। सम्वत में अमावस्या को अंत होने वाले माह (अमावस्यांत माह ) या पूर्णिमा को अंत होने वाले माह (पूर्णिमांत) माह कहा जाता है। किसी सम्वत में पूर्णिमांत माह का प्रयोग होता है और किसी में अमावस्यांत का। भारत के अलग अलग स्थानों पर एक ही नाम की सम्वत परम्परा में पूर्णिमांत या अमावस्यांत माह का प्रयोग हो सकता है। विक्रमी सम्वत का आरम्भ चैत्र माह के शुक्ल पक्ष से होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष दिवाली के अगले दिन आरम्भ होता है, इस दिन से वर्ष का आरंभ होने वाले सम्वत को विक्रमी सम्वत (कर्तक ) कहा जाता है।
सम्वत के अनुसार एक वर्ष की अवधि को भी सम्वत कहा जा सकता है।
सूर्य सिद्धांत
सूर्य सिद्धान्त भारतीय खगोलशास्त्र का प्रसिद्ध ग्रन्थ है। कई सिद्धान्त-ग्रन्थों के समूह का नाम है। वर्तमान समय में उपलब्ध ग्रन्थ मध्ययुग में रचित ग्रन्थ लगता है किन्तु अवश्य ही यह ग्रन्थ पुराने संस्क्रणों पर आधारित है जो ६वीं शताब्दी के आरम्भिक चरण में रचित हुए माने जाते हैं। भारतीय गणितज्ञों और खगोलशास्त्रियों ने इसका सन्दर्भ भी लिया है, जैसे आर्यभट्ट और वाराहमिहिर, आदि।
वाराहमिहिर ने अपने पंचसिद्धांतिका में चार अन्य टीकाओं सहित इसका उल्लेख किया है, जो हैं….
- पैतामाह सिद्धान्त : जो कि परम्परागत वेदांग ज्योतिष से अधिक समान है
- पौलिष सिद्धान्त
- रोमक सिद्धान्त : जो यूनानी खगोलशास्त्र के समान है
- वशिष्ठ सिद्धान्त : सूर्य सिद्धान्त नामक वर्णित कार्य, कई बार ढाला गया है। इसके प्राचीनतम उल्लेख बौद्ध काल (तीसरी शताब्दी, ई.पू) के मिलते हैं। वह कार्य, संरक्षित करके और सम्पादित किया हुआ (बर्गस द्वारा १८५८ में) मध्य काल को संकेत करता है। वाराहमिहिर का दसवीं शताब्दी के एक टीकाकार, ने सूर्य सिद्धांत से छः श्लोकों का उद्धरण किया है, जिनमें से एक भी अब इस सिद्धांत में नहीं मिलता है। वर्तमान सूर्य सिद्धांत को तब वाराहमिहिर को उपलब्ध उपलब्ध पाठ्य का सीधा वंशज माना जा सकता है। इसमें वे नियम दिये गये हैं, जिनके द्वारा ब्रह्माण्डीय पिण्डों की गति को उनकी वास्तविक स्थिति सहित जाना जा सकता है। यह विभिन्न तारों की स्थितियां, चांद्रीय नक्षत्रों के सिवाय; की स्थिति का भी ज्ञान कराता है। इसके द्वारा सूर्य ग्रहण का आकलन भी किया जा सकता है।
- मध्यमाधिकारः ग्रहों की चाल
- स्पष्टाधिकारः ग्रहों की स्थिति
- त्रिप्रश्नाधिकारः दिशा, स्थान और समय
- चन्द्रग्रहणाधिकारः चंद्रमा और ग्रहण
- सूर्यग्रहणाधिकारः सूर्य और ग्रहण
- छेद्यकाधिकारः ग्रहणों का पूर्व अनुमान/ आकलन
- ग्रहयुत्यधिकारः ग्रहीय संयोग
- भग्रहयुत्यधिकारः तारों के बारे में
- उदयास्ताधिकारः उनका उदय और अस्त
- चन्द्रशृंगोन्नत्यधिकारः चंद्रमा का उदय और अस्त
- पाताधिकारः सूर्य और चंद्रमा के एकई अहितकर पक्ष
- भूगोलाध्यायः विश्वोत्पत्ति/ब्रह्माण्ड सृजन, भूगोल और सृजन के आयाम
- ज्यौतिषोपनिषदध्यायः सूर्य घड़ी का दण्ड
- मानाध्यायः लोकों की गति और मानवीय क्रिया-कलाप
- सौर घड़ी द्वारा समय मापन के शुद्ध तरीके।
ग्रहों की चाल
भगण
- – १२ राशियो का एक भगण होता है ।
- – ६० विकला की एक कला ।
- – ६० कला का – १ अंश ।
- – ३० अंश को – १ राशि ।
- – शीघ्रगति वाले ग्रह अल्पकाल मे तथा मंद गतिवाले अधिक काल मे २७ नक्षत्र का भोग करते है ।
- – अश्विनी नक्षत्र सें भ्रमण करते हुये रेवती नक्षत्र तक ग्रहो का भगण पुरा होता है ।
- – पुर्वाभिमुख गमन करने वाले सुर्य-बुध और शुक्र और मंगल शनि और गुरू की भगण संख्या ४३२०००० होती है ।
- – एक महायुग मे चंद्रमा कि भगण संख्या – ५७७५३३३६,
- – एक महायुग मे मंगल कि भगण संख्या – २२९६८३२,
- – एक महायुग मे बुध कि भगण संख्या – १७९३७०६०,
- – एक महायुग मे गुरु की भगण संख्या – ३६४२२०
- – एक महायुग मे शुक्र की भगण संख्या – ७०२२३७६
- – एक महायुग मे शनि की भगण संख्या – १४६५६८
- – चंद्र की भगण संख्या – ४८८२०३
- – राहु-केतु की विपरीत गति से भगणों कि – २३२२३६ संख्या होती है ।
- – एक महायुग मे नक्षत्रो की भगण संख्या – १५८२२३७८२८ होती है ।
- – नाक्षत्र भगण मे से ग्रहो के अपने अपने भगण घटाने पर शेष ग्रहों के सावन दिन होते है।
- – एक महायुग मे सुर्य और चंद्रमा के भगणों के अंतर के समान चांद्रमास होते है।
- – युग चांद्रमास से युग सुर्य मास घटाने पर अधिमास मिलता है ।
- – एक महायुग में १५७७९१७८२८ सावन दिन होते है ।
- – १६०३००००८० तिथियाँ होती है ।
- – १५९३३३६ आधिमास होते है ।
- – २५०८२२५२ क्षय दिन होते है ।
- – ५१८४०००० सौर मास होते है ।
नक्षत्र भगण से सौर भगण घटाने पर सावन होता है ।
समय चक्र
हिन्दू ब्रह्माण्डीय समय चक्र सूर्य सिद्धांत के पहले अध्याय के श्लोक ११ से २३ में आते हैं।
- (श्लोक ११) – वह जो कि श्वास (प्राण) से आरम्भ होता है, यथार्थ कहलाता है; और वह जो त्रुटि से आरम्भ होता है, अवास्तविक कहलाता है। छः श्वास से एक विनाड़ी बनती है। साठ श्वासों से एक नाड़ी बनती है।
- (श्लोक १२) – और साठ नाड़ियों से एक दिवस (दिन और रात्रि) बनते हैं। तीस दिवसों से एक मास (महीना) बनता है। एक नागरिक (सावन) मास सूर्योदयों की संख्याओं के बराबर होता है।
- (श्लोक १३) – एक चंद्र मास, उतनी चंद्र तिथियों से बनता है। एक सौर मास सूर्य के राशि में प्रवेश से निश्चित होता है। बारह मास एक वरष बनाते हैं। एक वरष को देवताओं का एक दिवस कहते हैं।
- (श्लोक १४) – देवताओं और दैत्यों के दिन और रात्रि पारस्परिक उलटे होते हैं। उनके छः गुणा साठ देवताओं के (दिव्य) वर्ष होते हैं। ऐसे ही दैत्यों के भी होते हैं।
- (श्लोक १५) – बारह सहस्र (हज़ार) दिव्य वर्षों को एक चतुर्युग कहते हैं। एक चतुर्युग तिरालीस लाख बीस हज़ार सौर वर्षों का होता है।
- (श्लोक १६) – चतुर्युगी की उषा और संध्या काल होते हैं। कॄतयुग या सतयुग और अन्य युगों का अन्तर, जैसे मापा जाता है, वह इस प्रकार है, जो कि चरणों में होता है:
- (श्लोक १७) – एक चतुर्युगी का दशांश को क्रमशः चार, तीन, दो और एक से गुणा करने पर कॄतयुग और अन्य युगों की अवधि मिलती है। इन सभी का छठा भाग इनकी उषा और संध्या होता है।
- (श्लोक १८) – इकहत्तर चतुर्युगी एक मन्वन्तर या एक मनु की आयु होते हैं। इसके अन्त पर संध्या होती है, जिसकी अवधि एक सतयुग के बराबर होती है और यह प्रलय होती है।
- (श्लोक १९) – एक कल्प में चौदह मन्वन्तर होते हैं, अपनी संध्याओं के साथ; प्रत्येक कल्प के आरम्भ में पंद्रहवीं संध्या/उषा होती है। यह भी सतयुग के बराबर ही होती है।
- (श्लोक २०) – एक कल्प में, एक हज़ार चतुर्युगी होते हैं और फ़िर एक प्रलय होती है। यह ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसके बाद इतनी ही लम्बी रात्रि भी होती है।
- (श्लोक २१) – इस दिन और रात्रि के आकलन से उनकी आयु एक सौ वर्ष होती है; उनकी आधी आयु निकल चुकी है और शेष में से यह प्रथम कल्प है।
- (श्लोक २२) – इस कल्प में, छः मनु अपनी संध्याओं समेत निकल चुके, अब सातवें मनु (वैवस्वत: विवस्वान (सूर्य) के पुत्र) का सत्तैसवां चतुर्युगी बीत चुका है।
- (श्लोक २३) – वर्तमान में, अट्ठाईसवां चतुर्युगी का कॄतयुग बीत चुका है।……..
इस खगोलीय समय चक्र का आकलन करने पर, निम्न परिणाम मिलते हैं
उष्णकटिबनधीय वर्ष की औसत लम्बाई है ३६५.२४२१७५६ दिवस, जो कि आधुनिक आकलन से केवल १.४ सैकण्ड ही छोटी है। यह उष्णकटिबन्धीय वर्ष का सर्वाधिक विशुद्ध आंकलन रहा कम से कम अगली छः शताब्दियों तक, जब मुस्लिम गणितज्ञ उमर खय्याम ने एक बेहतर अनुमान दिया. फ़िर भी यह आंकलन अभी भी विश्व में प्रचलित ग्रेगोरियन वर्ष के मापन से अति शुद्ध ही है, जो कि वर्शः की अवधि केवल ३६५.२४२५ दिवस ही बताता है, यथार्थ ३६५.२४२१७५६ दिवस के स्थान पर।
एक नाक्षत्रीय वर्ष की औसत अवधि, पृथ्वी के द्वारा, सूर्य की परिक्रमा में लगे समय अवधि ३६५.२५६३६२७दिवस होती है, जो कि आधुनिक मान ३६५.२५६३६३०५ दिवस के एकदम बराबर ही है। यह नाक्षत्रीय वर्ष का सर्वाधिक परिशुद्ध कलन यहा सहस्रों वर्ष तक.
नाक्षत्रीय वर्ष का दिया गया यथार्थ मान, वैसे उतना शुद्ध नहीं है। इसका मान ३६५.२५८७५६ दिवस दिया गया है, जो कि आधुनिक मान से ३ मिनट और २७ सैकण्ड कम है। यह इसलिये है, क्योंकि लेखक, या सम्पादक ने बाद में किये गये कलनों में हिन्दू ब्रह्माण्डीय समय चह्र की गणना से थोड़ा भिन्न हो कर यहां गणना की है। उसने शायद समय चक्र के जटिल गणना के आकलन को सही समझा नहीं है। सम्पादक ने सूर्य की औसत गति और समान परिशुद्धता का प्रयोग किया है, जो कि हिन्दू ब्रह्माण्डीय समय चक्र के आकलन से निम्न स्तर का है।
पृथ्वी गोल है
सर्वत्रैव महीगोले स्वस्थानम् उपरि स्थितम् ।
मन्यन्ते खे यतो गोलस् तस्य क्वोर्धवम् क्व वाधः ॥ (सूर्यसिद्धान्त १२.५३)
अर्थात इस गोलाकार धरती पर लोग अपने स्थान को सबसे ऊपर मानते हैं। किन्तु यह गोला तो आकाश में स्थित है, उसका उर्ध्व (ऊपर) क्या और नीचे क्या?
ग्रहों के व्यास
सूर्य सिद्धान्त में ग्रहों के व्यास की गणना भी की गयी है। बुध का व्यास ३००८ मील दिया गया है जो आधुनिक स्वीकृत मान (३०३२ मील्) से केवल १% कम है। इसके अलावा शनि, मंगल, शुक्र और बृहस्पति के व्यास की गणना भी की गयी है। शनि का व्यास ७३८८२ मील बताया गया है जो केवल १% अशुद्ध है। मंगल का व्यास ३७७२ मील बताया गया है जो लगभग ११% अशुद्ध है। शुक्र का व्यास ४०११ मील तथा बृहस्पति का व्यास ४१६२४ मील बताया गया है जो वर्तमान स्वीकृत मानों के लगभग आधे हैं।
त्रिकोणमिती
सूर्य सिद्धान्त आधुनिक त्रिकोणमिति का मूल है। सूर्य सिद्धान्त में वर्णित ज्या और कोटिज्या फलनों से ही आधुनिक साइन और कोसाइन नाम व्युत्पन्न हुए हैं ( जो भारत से अरब-जगत होते हुए यूरोप पहुँचे)। इतना ही नहीं, सूर्यसिद्धान्त के तृतीय अध्याय (त्रिप्रश्नाधिकारः) में ही सबसे पहले स्पर्शज्या और व्युकोज्या का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित श्लोकों में शंकुक द्वारा निर्मित छाया का वर्णन करते हुए इनका उपयोग हुआ है-
शेषम् नताम्शाः सूर्यस्य तद्बाहुज्या च कोटिज्या।
शंकुमानांगुलाभ्यस्ते भुजत्रिज्ये यथाक्रमम् ॥ ३.२१ ॥
कोटिज्यया विभज्याप्ते छायाकर्णाव् अहर्दले।
क्रान्तिज्या विषुवत्कर्णगुणाप्ता शंकुजीवया ॥ ३.२२ ॥
कैलेण्डरीय प्रयोग
भारत के विभिन्न भागों में भारतीय सौर पंचांग तथा चन्द्र-सौर पंचांग प्रयुक्त होते हैं। इनके आधार पर ही विभिन्न त्यौहार, मेले, क्रियाकर्म होते हैं। भारत में प्रचलित आधुनिक सौर तथा चान्द्रसौर पंचांग, सूर्य के विभिन्न राशियों में प्रवेश के समय पर ही आधारित हैं।
परम्परागत पंचांगकार, आज भी सूर्यसिद्धान्त में निहित सूत्रों और समीकरणों का ही प्रयोग करके अपने पंचांग का निर्माण करते हैं। भारतीयों के धार्मिक एवं सामाजिक जीवन पर पंचांग का बहुत अधिक प्रभाव है तथा अधिकांश घरों में पंचांग रखने की प्रथा है।
यंत्र
पारदाराम्बुसूत्राणि शुल्वतैलजलानि च।
बीजानि पांसवस्तेषु प्रयोगास्तेऽपि दुर्लभाः ॥१३.२२ ॥
अर्थात् : ताड़ियों में पारद भरा हुआ, जल, धागा (सूत्र), रस्सी, तेल और जल आदि से ये यंत्र बनाये जाते हैं। इसके अलावा बीज और महीन रेत भी इन यंत्रों में प्रयुक्त होती हैं। ये यन्त्र दुर्लभ हैं।
॥ श्रीरस्तु ॥
❀꧁꧂❀
श्री हरि हरात्मक देवें सदा, मुद मंगलमय हर्ष।
सुखी रहे परिवार संग, अपना भारतवर्ष ॥
❀꧁꧂❀
संकलनकर्ता –
श्रद्धेय पंडित विश्वनाथ द्विवेदी ‘वाणी रत्न’
संस्थापक, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
(‘हरि हर हरात्मक’ ज्योतिष)
संपर्क सूत्र – 07089434899
┉┅━❀꧁꧂❀━┅┉
Share this content:





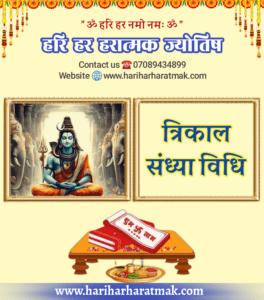


Post Comment